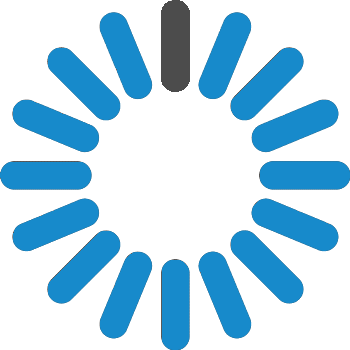एक नजर
- कृषि क्षेत्र में देश की लगभग आधी श्रमशक्ति कार्यरत है। हालांकि जीडीपी में इसका योगदान 17.5% है (2015-16 के मौजूदा मूल्यों पर)।
- पिछले कुछ दशकों के दौरान, अर्थव्यवस्था के विकास में मैन्यूफैक्चरिंग और सेवा क्षेत्रों का योगदान तेजी से बढ़ा है, जबकि कृषि क्षेत्र के योगदान में गिरावट हुई है। 1950 के दशक में जीडीपी में कृषि क्षेत्र का योगदान जहां 50% था, वहीं 2015-16 में यह गिरकर 15.4% रह गया (स्थिर मूल्यों पर)।
- भारत का खाद्यान्न उत्पादन प्रत्येक वर्ष बढ़ रहा है और देश गेहूं, चावल, दालों, गन्ने और कपास जैसी फसलों के मुख्य उत्पादकों में से एक है। यह दुग्ध उत्पादन में पहले और फलों एवं सब्जियों के उत्पादन में दूसरे स्थान पर है। 2013 में भारत ने दाल उत्पादन में 25% का योगदान दिया जोकि किसी एक देश के लिहाज से सबसे अधिक है। इसके अतिरिक्त चावल उत्पादन में भारत की हिस्सेदारी 22% और गेहूं उत्पादन में 13% थी। पिछले अनेक वर्षों से दूसरे सबसे बड़े कपास निर्यातक होने के साथ-साथ कुल कपास उत्पादन में भारत की हिस्सेदारी 25% है।
- हालांकि अनेक फसलों के मामलों में चीन, ब्राजील और अमेरिका जैसे बड़े कृषि उत्पादक देशों की तुलना में भारत की कृषि उपज कम है (यानी प्रति हेक्टेयर जमीन में उत्पादित होने वाली फसल की मात्रा)।
|
||||||
- ऐसे कई कारण हैं, जोकि कृषि उत्पादकता को प्रभावित करते हैं, जैसे खेती की जमीन का आकार घट रहा है और किसान अब भी काफी हद तक मानसून पर निर्भर हैं। सिंचाई की पर्याप्त सुविधा नहीं है, साथ ही उर्वरकों का असंतुलित प्रयोग किया जा रहा है जिससे मिट्टी का उपजाऊपन कम होता है। देश के विभिन्न भागों में सभी को आधुनिक तकनीक उपलब्ध नहीं है, न ही कृषि के लिए औपचारिक स्तर पर ऋण उपलब्ध हो पाता है। सरकारी एजेंसियों द्वारा खाद्यान्नों की पूरी खरीद नहीं की जाती है और किसानों को लाभकारी मूल्य नहीं मिल पाते हैं।
- इस संबंध में कमिटियों और एक्सपर्ट संस्थाओं द्वारा पिछले कई वर्षों से अनेक सुझाव दिए जा रहे हैं, जैसे कृषि की जमीन की पट्टेदारी के कानून बनाना, कुशलतापूर्वक पानी का उपयोग करने के लिए लघु सिंचाई तकनीक को अपनाना, निजी क्षेत्र को संलग्न करते हुए अच्छी क्वालिटी के बीजों तक पहुंच को सुधारना और कृषि उत्पादों की ऑनलाइन ट्रेडिंग के लिए राष्ट्रीय कृषि बाजार की शुरुआत करना।
भारत में कृषि की स्थिति
कृषि उत्पादकता कई कारकों पर निर्भर करती है। इनमें कृषि इनपुट्स, जैसे जमीन, पानी, बीज एवं उर्वरकों की उपलब्धता और गुणवत्ता, कृषि ऋण एवं फसल बीमा की सुविधा, कृषि उत्पाद के लिए लाभकारी मूल्यों का आश्वासन, और स्टोरेज एवं मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इत्यादि शामिल हैं। यह रिपोर्ट भारत में कृषि की स्थिति का विवरण प्रस्तुत करती है। इसके अतिरिक्त कृषि उत्पादन और पैदावार के बाद की गतिविधियों से संबंधित कारकों पर चर्चा करती है।
2009-10 तक देश की आधी से अधिक श्रमशक्ति (53%), यानी 243 मिलियन लोग कृषि क्षेत्र में कार्यरत थे।[1] इस क्षेत्र से अपनी आजीविका कमाने वाले लोगों में भूस्वामी, काश्तकार, जोकि जमीन के एक टुकड़े में खेती करते हैं, और खेत मजदूर, जो इन खेतों में मजदूरी करते हैं, शामिल हैं। पिछले 10 वर्षों के दौरान कृषि उत्पादन अस्थिर रहा है, इसकी वार्षिक वृद्धि 2010-11 में 8.6%, 2014-15 में -0.2% और 2015-16 में 0.8% थी।[2] रेखाचित्र 3 में पिछले 10 वर्षों के दौरान कृषि क्षेत्र में वृद्धि की प्रवृत्तियों को प्रदर्शित किया गया है।
|
रेखाचित्र 3: कृषि में वृद्धि (%) स्रोत: एक नजर में कृषि सांख्यिकी, 2015, कृषि मंत्रालय; पीआरएस। |
रेखाचित्र 4: विभिन्न क्षेत्रों का जीडीपी में योगदान (%) स्रोत: सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय; पीआरएस। |
जैसा कि रेखाचित्र 4 में प्रदर्शित किया गया है, सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में कृषि क्षेत्र का योगदान कम हुआ है। यह 1950-1951 में 54% से गिरकर 2015-16 में 15.4% हो गया, जबकि सेवा क्षेत्र 30% से बढ़कर 53% हो गया।[3],2जहां जीडीपी में कृषि क्षेत्र के योगदान में पिछले कुछ दशकों में गिरावट हुई है, मैन्यूफैक्चरिंग (10.5% आबादी कार्यरत) और सेवा (24.4% आबादी कार्यरत) क्षेत्रों का योगदान बढ़ा है।1
कृषि उत्पादन और उपज
तालिका 5 में पिछले कुछ दशकों में फसल उत्पादन के आंकड़े प्रदर्शित किए गए हैं। परिशिष्ट में प्रस्तुत तालिका 7 पिछले कुछ दशकों के दौरान मुख्य फसलों के उत्पादन को प्रदर्शित करती है।
|
रेखाचित्र 5: कृषि उत्पादन (मिलियन टन) स्रोत: कृषि मंत्रालय; पीआरएस। |
· खाद्यान्नों का कुल उत्पादन 1950-51 में 51 मिलियन टन से बढ़कर 2015-16 में 252 मिलियन टन हो गया।[4] कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमानों के अनुसार, 2016-17 में 272 मिलियन टन के खाद्यान्न उत्पादन का अनुमान है।[5] · 1960 के दशक में हरित क्रांति के बाद गेहूं और चावल के उत्पादन में जबरदस्त वृद्धि हुई और 2015-16 तक, देश के कुल खाद्यान्न उत्पादन में गेहूं और चावल की हिस्सेदारी 78% हो गई। |
अपनी आबादी का पेट भरने के लिए 2025 तक देश को 300 मिलियन टन खाद्यान्न की आवश्यकता होगी, ऐसा अनुमान लगाया गया है।[6] 2015-16 में 252 मिलियन टन खाद्यान्न उत्पादन का अनुमान है। इसका अर्थ यह है कि फसल उत्पादन में औसत 2% की वार्षिक वृद्धि अपेक्षित है जोकि वृद्धि की मौजूदा प्रवृत्ति के बहुत निकट है।
उत्पादन के उच्च स्तरों के बावजूद भारत में अन्य बड़े उत्पादक देशों की तुलना में कृषि उपज कम है। कृषि उपज प्रति हेक्टेयर जमीन में उत्पादित होने वाली फसल की मात्रा होती है। 1950-51 से खाद्यान्नों की उपज में चार गुना वृद्धि हुई है। 2014-15 के दौरान यह 2,071 किलो प्रति हेक्टेयर था।[7] जैसा कि रेखाचित्र 6 में प्रदर्शित किया गया है कि चीन, ब्राजील और अमेरिका जैसे देशों की तुलना में भारत की उपज कम है।
|
रेखाचित्र 6: 2014-15 के दौरान विभिन्न देशों में उपज (टन प्रति हेक्टेयर में) स्रोत: संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन; पीआरएस। |
· हालांकि भारत विश्व में धान (चावल) का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है (2013 तक), फिर भी उसकी उपज चीन, ब्राजील और अमेरिका से कम है। यही स्थिति दाल उत्पादन की भी है। दालों के प्रमुख उत्पादकों में से एक होने के बावजद उसकी उपज सबसे कम है।[8],[9] · अन्य देशों की तुलना में भारत में कृषि उत्पादकता की वृद्धि दर बहुत धीमी रही है। उदाहरण के लिए ब्राजील में चावल की उपज 1981 में 1.3 टन प्रति हेक्टेयर थी, जोकि 2011 में बढ़कर 4.9 टन प्रति हेक्टेयर हो गई। इसके मुकाबले भारत की उपज 2.0 टन प्रति हेक्टेयर से बढ़कर 3.6 टन प्रति हेक्टेयर हो गई। इस अवधि में चीन में चावल की उत्पादकता भी 4.3 टन प्रति हेक्टेयर से बढ़कर 6.7 टन प्रति हेक्टेयर हो गई।
|
खाद्य सुरक्षा और पोषण
किसानों और मजदूरों को आजीविका प्रदान करने के अतिरिक्त कृषि क्षेत्र देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करता है। संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन (एफएओ) के अनुसार, खाद्य सुरक्षा वह स्थिति है, जब सभी लोगों को, हर समय, पर्याप्त, सुरक्षित और ऐसा पौष्टिक भोजन प्राप्त होता है, जोकि स्वस्थ और सक्रिय जीवन के लिए उनकी आहार संबंधी जरूरतों और भोजन संबंधी प्राथमिकताओं को पूरा करता हो।[10] देश में उच्च उत्पादन के बावजूद 2014 के अनुमान बताते हैं कि 15% लोग अब भी कुपोषण का शिकार हैं।[11],[12]
2013 में भारत ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एक्ट लागू किया। इस एक्ट का उद्देश्य सस्ती कीमतों पर पर्याप्त मात्रा में अच्छे भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित करते हुए लोगों को खाद्य और पोषण सुरक्षा प्रदान करना है।[13] 2013 के एक्ट के तहत विशेष श्रेणियों के लोगों को रियायती कीमतों पर खाद्यान्न (गेहूं, चावल और मोटे अनाज) दिए जाते हैं। 2015 तक 68%, यानी 81 करोड़ लोग (जिनमें से 77% ग्रामीण और 23% शहरी क्षेत्रों में आते हैं) इस एक्ट के दायरे में आते हैं।[14]
पिछले कुछ दशकों में प्रति व्यक्ति आय और अनेक प्रकार के खाद्य समूहों की उपलब्धता के बढ़ने के साथ देश में खाद्य पदार्थों के उपभोग का पैटर्न बदल रहा है। पोषण के लिए अनाज पर निर्भरता घटी है और प्रोटीन के उपभोग में वृद्धि हुई है।[15] प्रोटीन के स्रोतों में दालें, मांस, समुद्री खाद्य (सीफूड), अंडे इत्यादि शामिल हैं। देश में दालों के उत्पादन को बढ़ावा देने पर केंद्रित वित्त मंत्रालय की एक रिपोर्ट के अनुसार, प्रोटीन के उपभोग को बढ़ाना सरकार की नीतिगत प्राथमिकता होनी चाहिए।[16] रिपोर्ट के अनुसार, प्रोटीन के तमाम स्रोतों की तुलना में दाल की कीमत कम है। मौजूदा घरेलू परिदृश्य में भारत में दालों की कमी है जिसकी भरपाई आयात के जरिए से की जाती है।
कृषि व्यापार
भारत में आयात होने वाली मुख्य वस्तुओं में दालें, खाद्य तेल, ताजा फल और काजू हैं। भारत द्वारा जिन प्रमुख वस्तुओं का निर्यात किया जाता है, उनमें चावल, मसाले, कपास, मांस और मांस से बने खाद्य, चीनी इत्यादि शामिल हैं। पिछले कुछ दशकों में कुल आयात में कृषि आयात की हिस्सेदारी 1990-91 में 2.8% से बढ़कर 2014-15 में 4.2% हो गई, जबकि कृषि निर्यात की हिस्सेदारी 18.5% से घटकर 12.7% हो गई।[17] तालिका 1 और 2 में पिछले तीन वर्षों के दौरान कुल कृषि निर्यात और आयात के आंकड़े प्रदर्शित किए गए हैं।
|
तालिका 1: कृषि निर्यात (बिलियन डॉलर में)
स्रोत: वार्षिक रिपोर्ट, वाणिज्य विभाग; पीआरएस। |
तालिका 2: कृषि आयात (बिलियन डॉलर में)
स्रोत: वार्षिक रिपोर्ट, वाणिज्य विभाग; पीआरएस। |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
भारत की व्यापार नीति वस्तुओं की घरेलू उपलब्धता, उत्पादन की लागत और विश्व स्तर पर उसके मूल्य स्तर जैसे कई कारकों से प्रभावित होती है।[18] हालांकि व्यापार नीति में निरंतर बदलावों जैसे आपूर्ति कम होने के कारण वस्तुओं के आयात शुल्क को कम करने या निर्यात बढ़ाने के लिए वस्तुओं के न्यूनतम निर्यात को मूल्य घटाने का कृषि प्रसंस्करण क्षेत्र के विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।18
कृषि उत्पादकता को प्रभावित करने वाले कारक
भूमि के छोटे स्वामित्व में वृद्धि
2012-13 तक 140 मिलियन हेक्टेयर भूमि को कृषि के लिए प्रयोग किया जा रहा था।[19] पिछले कुछ वर्षों के दौरान इस क्षेत्र को जमीन के छोटे टुकड़ों में खंडित कर दिया गया है। जैसा कि तालिका 3 में प्रदर्शित किया गया है, सीमांत स्वामित्व वाली जमीन की संख्या 1971 में 36 मिलियन से बढ़कर 2011 में 93 मिलियन हो गई।[20] सीमांत और छोटे स्वामित्व वाली जमीनों के साथ कई समस्याएं होती हैं, जैसे मशीनीकरण और सिंचाई की तकनीकों का प्रयोग करने से जुड़ी समस्याएं।
|
चूंकि छोटी जमीनें अक्सर बड़ी जमीनों का टुकड़ा होती हैं, जो एक परिवार के भीतर हस्तांतरित होती हैं या बड़े किसान द्वारा अनौपचारिक रूप से पट्टे पर दी जाती है, इन जमीनों पर खेती करने वाले किसानों के पास पट्टे का लिखित करारनामा (औपचारिक लीज एग्रीमेंट) नहीं होता है। भूमि रिकॉर्ड न होने के कारण इन किसानों को औपचारिक ऋण उपलब्ध नहीं होता या वे इनपुट सबसिडी या फसल बीमा योजनाओं जैसी सरकारी सुविधाओं के पात्र (एलिजिबल) नहीं होते।
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
भूमि के रिकॉर्ड और अनौपचारिक पट्टेदारी
|
कर्नाटक में ई-भूमि परियोजना कर्नाटक सरकार ने 2000 के प्रारंभ में ई-भूमि परियोजना की शुरुआत की। इस परियोजना का उद्देश्य मौजूद भूमि रिकॉर्डों का कंप्यूटरीकरण करना और भूमि रिकॉर्ड को बदलने एवं प्लॉटों को विभाजित या विलय करने के लिए एक पारदर्शी प्रणाली तैयार करना था। इस प्रणाली के तहत किसान तहसील के स्तर पर अपने प्लॉट से जुड़े रिकॉर्ड प्राप्त कर सकते हैं जिन्हें पहणि कहा जाता है। इन रिकॉर्डों में जमीन का सर्वे नंबर, भूस्वामी का विवरण, मिट्टी का प्रकार, सिंचाई और फसल से जुड़े विवरण इत्यादि शामिल होते हैं। पहणि से किसानों को निम्नलिखित लाभ मिलते हैं (i) उन्हें यह पता चलता है कि वे जिस प्लॉट को खरीदना चाहते हैं, वह सही है, (ii) इससे वे बैंक से ऋण ले सकते हैं, (iii) इन रिकॉर्डों का इस्तेमाल वे सरकारी या कानूनी काम के लिए कर सकते हैं। ई-भूमि के जरिए किसानों के लिए शिकायत निवारण हेतु सरकार से संपर्क करना आसान होता है। |
देश में जितनी भूमि पर खेती होती है, उसमें से 10% जमीन खेती करने के लिए पट्टे पर दी जाती है। विभिन्न राज्यों में पट्टेदारी का प्रतिशत अलग-अलग है।[21] जैसे आंध्र प्रदेश में 34%, पंजाब में 25%, बिहार में 21% और सिक्किम में 18% जमीन खेती के लिए पट्टे पर दी गई है। इससे पहले कर्नाटक और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में काश्तकारों को कानूनी अधिकार देने के प्रयास किए गए। वहां भूमि स्वामित्व का इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड तैयार किया गया और पैदावार पर काश्तकारों को अधिकार प्रदान किया गया।[22],[23]
वर्तमान में विभिन्न राज्यों में अलग-अलग काश्तकारी कानून हैं।21केरल, जम्मू एवं कश्मीर और मणिपुर में कृषि भूमि को पट्टे पर देना प्रतिबंधित है। बिहार, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना और ओड़िशा जैसे राज्यों में भूस्वामियों की कुछ ही श्रेणियों द्वारा जमीन पट्टे पर दी जा सकती है। दूसरी ओर गुजरात, महाराष्ट्र और असम जैसे राज्य स्पष्ट रूप से पट्टेदारी को प्रतिबंधित नहीं करते और काश्तकारी की एक निश्चित अवधि के बाद काश्तकार को भूस्वामी से जमीन खरीदने की अनुमति देते हैं। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में पट्टे पर जमीन देने पर कानूनी प्रतिबंध नहीं है। भिन्न-भिन्न राज्यों में पट्टे पर जमीन देने की अधिकतम सीमा भी अलग-अलग है।21
|
पश्चिम बंगाल में बरगादार प्रणाली पश्चिम बंगाल भूमि सुधार एक्ट, 1955 बरगादारों या काश्तकारों को कुछ अधिकार देता है। बरगादार वह व्यक्ति होता है, जो किसी अन्य व्यक्ति की जमीन पर कानूनन खेती करता है (जोकि उसके परिवार का सदस्य नहीं होता)। एक्ट के तहत कृषि उपज को काश्तकार और भूस्वामी के बीच 50:50 के अनुपात में बांटा जाता है, अगर बैल, खाद और बीज भूस्वामी द्वारा दिए जाएं और अन्य सभी मामलों में यह विभाजन 75:25 का होगा। एक्ट के तहत काश्तकार की बेदखली एक संज्ञेय अपराध है जिसके लिए कैद या जुर्माने का प्रावधान है। हालांकि इससे काश्तकार को स्वामित्व का अधिकार नहीं मिलता। |
नीति आयोग ने जमीन की पट्टेदारी को वैधता प्रदान करने के लिए एक मॉडल भूमि पट्टेदारी कानून प्रस्तावित किया है।21इससे भूस्वामियों के स्वामित्व अधिकारों और काश्तकारों के काश्तकारी अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी। काश्तकारी को वैधता मिलने से यह भी सुनिश्चित होगा कि किसानों को औपचारिक ऋण, बीमा, और इनपुट जैसे उर्वरकों की सुविधा उपलब्ध होगी। परिशिष्ट में प्रस्तुत तालिका 16 में पट्टेदारी से जुड़े प्रतिबंधों का विवरण है, साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि राज्यों ने किस हद तक मॉडल भूमि पट्टेदारी कानून को स्वीकार किया है।[24] केवल मध्य प्रदेश ने अब तक मॉडल भूमि पट्टेदारी कानून को स्वीकार किया है।
कृषि ऋण और बीमा की सुविधा
कृषि ऋण की सुविधा जमीन के स्वामित्व (होल्डिंग ऑफ लैंड टाइटिल) से जुड़ा हुआ मामला है। इसके परिणाम स्वरूप ऐसे छोटे और सीमांत किसान, जो देश में आधी से अधिक भूमि पर खेती करते हैं, औपचारिक भूमि स्वामित्व न होने के कारण संस्थागत ऋण की सुविधा प्राप्त नहीं कर पाते।[25] किसानों को दो प्रकार के ऋणों की जरूरत होती है। इनपुट्स खरीदने, निराई, कटाई, छंटाई और परिवहन के लिए उन्हें अल्प अवधि के ऋण की जरूरत हो सकती है और कृषि मशीनरी एवं उपकरण, या सिंचाई के लिए दीर्घावधि के ऋण की। तालिका 4 में 2013 तक ऋण स्रोतों के अनुसार कृषि ऋणों का वितरण किया गया है।
तालिका 4: भू स्वामित्व और कृषि ऋण के स्रोत (2013 तक)
|
भूमि का आकार (हेक्टेयर) |
को-ऑपरेटिव सोसायटी |
बैंक |
साहूकार |
दुकानदार/व्यापारी |
संबंधी/मित्र |
अन्य |
|
0-1 |
10% |
27% |
41% |
4% |
14% |
4% |
|
1-2 |
15% |
48% |
23% |
2% |
8% |
6% |
|
2-4 |
16% |
50% |
24% |
1% |
6% |
4% |
|
4-10 |
18% |
50% |
19% |
1% |
7% |
6% |
|
10+ |
14% |
64% |
16% |
1% |
4% |
2% |
स्रोत: तालिका 3.2, वित्तीय समावेश पर मध्यम अवधि मार्ग संबंधी कमिटी की रिपोर्ट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया; पीआरएस।
एक हेक्टेयर से कम जमीन वाले किसान अधिकतर ऋण के अनौपचारिक स्रोतों, जैसे साहूकारों से ऋण लेते हैं (41%), जबकि दो हेक्टेयर या उससे अधिक की जमीन वाले किसान मुख्य रूप से बैंकों से उधार लेते हैं (50% या उससे अधिक)। कृषि ऋण के प्रमुख स्रोतों में दुकानदार, संबंधी या मित्र, और को-ऑपरेटिव सोसायटियां शामिल हैं। कृषि ऋण से जुड़ी कई समस्याएं हैं जैसे स्पष्ट भूमि रिकॉर्ड न होने कारण औपचारिक ऋण न मिलना, अल्पावधि और दीर्घावधि के कृषि ऋणों का विषम अनुपात और फसल बीमा उपलब्ध न होना। यहां संक्षेप में इसका ब्यौरा दिया जा रहा है।25
अल्पावधि और दीर्घावधि के ऋण
सामान्य तौर पर अल्पावधि के ऋण पैदावार से पहले और उसके बाद की गतिविधियों जैसे निराई, कटाई, छंटाई और परिवहन हेतु लिए जाते हैं। दूसरी ओर कृषि मशीनरी एवं उपकरण, सिंचाई और विकास की अन्य गतिविधियों इत्यादि के लिए दीर्घावधि के ऋण लिए जाते हैं। पिछले कुछ दशकों के दौरान देश में अल्पावधि और दीर्घावधि के ऋणों की प्रवृत्ति उलट गई है। 1990-91 में अधिकतर कृषि ऋण दीर्घावधि के होते थे, जबकि कुल कृषि ऋणों में अल्पावधि के ऋणों का हिस्सा सिर्फ एक चौथाई होता था।[26] 2011-12 में 61% कृषि ऋण अल्पावधि के थे, जबकि दीर्घावधि के ऋणों का हिस्सा 39% था। [27]
इसके अतिरिक्त छोटे और सीमांत किसान, जिनका 86% स्वामित्व कुल कृषि भूमि पर है, मध्यम और बड़े स्वामित्व वाले किसानों की तुलना में अल्पावधि के ऋण अधिक लेते हैं। अनौपचारिक स्रोतों जैसे साहूकारों, परिवार के सदस्यों और मित्रों से ऋण लेने के मामलों में भी ऐसे किसानों की हिस्सेदारी सबसे अधिक है।
फसल बीमा तक पर्याप्त पहुंच न होना
2011 तक केवल 10% भारतीय किसानों को फसल बीमा योजना का लाभ मिला था।[28] फसल बीमा प्रणाली से जुड़ी स्थायी समस्याएं निम्नलिखित हैं (i) बीमा योजनाओं के बारे में जानकारी न होना, (ii) बीमा योजनाओं का पर्याप्त कवरेज न होना, (iii) फसल का नुकसान होने पर यह आकलन करना कि नुकसान किस हद तक हुआ है, और (iv) एक निश्चित समय में दावों का निपटारा।[29]
वित्त संबंधी स्टैंडिंग कमिटी ने सुझाव दिया था कि फसल के नुकसान का आकलन और किसान के खाते में मुआवजे को सीधे हस्तांतरित करने का काम एक निश्चित समय में पूरा किया जाना चाहिए।29 इसके अतिरिक्त अनुत्पादक ऋणों को कम करने के लिए सरकार को इस संबंध में जागरूकता फैलानी चाहिए कि विभिन्न क्षेत्रों में मिट्टी की क्वालिटी और बारिश इत्यादि के आधार पर किस प्रकार की फसल उगाई जाए।29
|
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जनवरी 2016 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को केंद्र सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया था।[30] इस योजना का लक्ष्य फसल का नुकसान होने की स्थिति में किसानों को बीमा लाभ देना, किसानों की आय को स्थिर बनाना और किसानों को खेती के आधुनिक तौर-तरीके अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना, इत्यादि है। 2016-17 में इस योजना के लिए केंद्रीय बजट में 5,501 करोड़ रुपए आबंटित किए गए थे, जिसे 2017-18 में बढ़ाकर 9,000 करोड़ रुपए कर दिया गया।[31],[32]इस योजना के अंतर्गत अधिसूचित क्षेत्रों में अधिसूचित फसल उगाने वाले सभी किसान आते हैं, जिसमें काश्तकार और बटाईदार किसान भी शामिल हैं। अधिसूचित फसलों में अनाज, दालें, तिलहन, सब्जियां, मसाले इत्यादि शामिल हैं। दिसंबर 2016 तक इस योजना में उस वर्ष के खरीफ मौसम में 1,41,625 करोड़ रुपए की राशि के साथ 367 लाख किसान शामिल थे, जबकि 2015 के खरीफ मौसम में 69,307 करोड़ रुपए की राशि के साथ 309 लाख किसान शामिल थे।[33],[34],[35] |
भारतीय रिजर्व बैंक के तहत वित्तीय समावेश संबंधी कमिटी ने सुझाव दिया कि काश्तकारों को ऋण योग्यता सर्टिफिकेट जारी किए जाने चाहिए जोकि काश्तकारी/पट्टा सर्टिफिकेट के तौर पर काम करेंगे।25इन सर्टिफिकेट्स से भूमिहीन किसानों को कृषि ऋण मिल सकेगा। कमिटी ने सुझाव दिया कि भारतीय रिजर्व बैंक को बैंकों को इस संबंध में दिशानिर्देश जारी करने चाहिए कि इन सर्टिफिकेट्स के बदले किसानों को ऋण दिए जाएं।
पानी की उपलब्धता
वर्तमान में खाद्यान्न की पैदावार करने वाली लगभग 51% कृषि भूमि में सिंचाई की जाती है।[36] बाकी का क्षेत्र बारिश पर निर्भर है (वर्षा आधारित कृषि)। सिंचाई के स्रोतों में भूजल (कुएं, ट्यूबवेल) और सतही जल (नहर, टैंक) शामिल है। तालिका 5 कृषि में प्रयोग किए जाने वाले सिंचाई के स्रोतों को प्रदर्शित करती है।
तालिका 5: सिंचाई के स्रोत (2010-11 तक)
स्रोत: कृषि गणना 2011; पीआरएस। |
· पानी को अधिक कुशलता से उपयोग किए जाने की जरूरत है, खासकर खेती में। वर्तमान में सिंचाई में देश का 84% कुल उपलब्ध पानी प्रयोग किया जाता है।[37] · लगभग 65% सिंचित कृषि भूमि की सिंचाई के लिए भूजल स्रोतों जैसे ट्यूबवेल और कुओं का उपयोग किया जाता है। |
पिछले कुछ दशकों में कई राज्यों में भूजल स्रोतों का अत्यधिक उपयोग किया गया है, विशेष रूप से ऐसे राज्य जिनमें वर्षा गहन फसलें जैसे चावल, उगाई जाती हैं। उदाहरण के लिए हरियाणा और राजस्थान में 40% से 75% भूजल इकाइयों का अति दोहन किया गया है, और पंजाब में स्थिति और बदतर है, जहां 75% से 90% इकाइयों का अति दोहन किया गया है।[38] विभिन्न राज्यों में भूजल विकास का विवरण परिशिष्ट की तालिका 15 में देखा जा सकता है।
कृषि लागत और मूल्य आयोग ने सुझाव दिया है कि पानी के प्रत्येक हेक्टेयर उपयोग की एक सीमा तय कर दी जानी चाहिए।[39] इसके अतिरिक्त निर्धारित सीमा से कम पानी उपयोग करने वाले किसानों को मौजूदा घरेलू लागत पर पानी की बची हुई यूनिट्स के बदले रुपए दिए जाने चाहिए। इससे वे पानी को कम उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित होंगे।
2011 और 2013 में सरकार ने भूजल प्रबंधन के लिए मॉडल बिल पेश किए जिसके आधार पर राज्य अपने कानून बना सकते हैं।[40] सरकार ने 2012 में जल मांग प्रबंधन, पानी के कुशलतापूर्ण उपयोग और मूल्य से संबंधित एक नीति की शुरुआत भी की।[41] म़ॉडल बिल सार्वजनिक न्यास सिद्धांत (पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन) पर आधारित थे, जिसके तहत सार्वजनिक प्रयोग के लिए निर्धारित संसाधनों को निजी स्वामित्व में नहीं बदला जा सकता। हाल ही में जल संसाधन मंत्रालय ने भूजल के लिए मॉडल बिल, 2016 का वितरण किया है जिसे राज्यों द्वारा स्वीकृत किया जा सकता है।[42] बिल भूजल के संरक्षण और प्रबंधन के लिए संस्थागत संरचना प्रदान करता है। बिल कहता है कि भूजल सभी लोगों के लिए एक समान संसाधन है और अगर किसी का स्वामित्व उस जमीन पर है जिसके नीचे कोई भूजल संसाधन है तो इसका यह अर्थ नहीं कि दूसरों को भूजल से वंचित किया जाए। इसमें यह भी कहा गया है कि भूजल के औद्योगिक और थोक में उपयोग का मूल्य निर्धारित किया जाएगा।
सूक्ष्म सिंचाई तकनीक
आर्थिक सर्वेक्षण 2015-16 में कहा गया है कि भारत में फ्लड इरिगेशन (बाढ़ सिंचाई) की तकनीक को बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता है। इसमें खेतों में पानी को बहाया जाता है और इसके बाद पानी मिट्टी में रिस जाता है।[43] इससे पानी की बर्बादी होती है क्योंकि अतिरिक्त पानी मिट्टी में रिस जाता है या बिना इस्तेमाल हुए सतह पर बह जाता है। यह सुझाव दिया गया कि किसानों को बाढ़ सिंचाई की बजाय टपक या बौछार सिंचाई प्रणाली (ड्रिप या स्प्रिंक्लर इरिगेशन सिस्टम्स) (सूक्ष्म सिंचाई) का इस्तेमाल करना चाहिए।[44] इससे पानी का संरक्षण तो होगा ही, साथ ही सिंचाई पर लगने वाले धन की बचत भी होगी। सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली का प्रयोग करने से (जैसे टपक या बौछार सिंचाई) उपज भी बढ़ती है।
उल्लेखनीय है कि चीन, ब्राजील और अमेरिका जैसे देशों की तुलना में भारत में एक टन अनाज के उत्पादन में 2 से 3 गुना अधिक पानी का उपयोग किया जाता है।43अगर भारत में भी पानी का कुशलतापूर्वक उपयोग किया जाता है तो अधिक व्यापक क्षेत्र में सिंचाई करना आसान होगा। परिशिष्ट की तालिका 14 में देश में सूक्ष्म सिंचाई के राज्य वार कवरेज को प्रदर्शित किया गया है।
मिट्टी और उर्वरक
मिट्टी की क्वालिटी
मिट्टी कृषि उत्पादकता का एक महत्वपूर्ण घटक है। भारत में मिट्टी में मुख्य रूप से नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एवं पोटाशियम जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त द्वितीयक पोषक तत्व सल्फर, कैलशियम एवं मैग्नीशियम और सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे जिंक, आयरन और मैगनीज इत्यादि पाए जाते हैं।[45] हालांकि पिछले कुछ दशकों में खाद्य उत्पादन का स्तर बढ़ा है लेकिन इसके साथ कई समस्याएं भी खड़ी हुई हैं जैसे मिट्टी में पोषक तत्वों का असंतुलन, जलस्तर एवं पानी की क्वालिटी का गिरना और मिट्टी के स्वास्थ्य का बिगड़ना।[46] 16.4 टन प्रति हेक्टेयर की दर से हर वर्ष लगभग 5.3 अरब टन मिट्टी नष्ट हो जाती है।
उर्वरकों का असंतुलित प्रयोग करने से मिट्टी का उपजाऊपन खत्म होता है। अगर किसानों को इस बात की जानकारी नहीं होगी कि जिस खेत में वे बुवाई करते हैं, उस खेत की मिट्टी के लिए किस प्रकार के उर्वरक की जरूरत है, तो मिट्टी की उत्पादकता पर असर होगा। 2015 में केंद्र सरकार ने मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के तहत सभी किसानों को हर तीन साल बाद मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जाते हैं। मृदा स्वास्थ्य कार्ड में मिट्टी में पोषक तत्वों की स्थिति की जानकारी के अतिरिक्त यह सुझाव भी दिया जाता है कि उपजाऊपन में सुधार करने के लिए कितने पोषक तत्व मिट्टी में मिलाए जाने चाहिए। इस योजना में फरवरी 2017 तक 2.9 करोड़ किसान शामिल किए गए थे।[47] मिट्टी के 2.5 करोड़ सैंपल इकट्ठे किए गए और 1.8 करोड़ सैंपलों की जांच की गई।[48] मंत्रालय ने मार्च 2017 तक 2.53 करोड़ सैंपल इकट्ठे करने का लक्ष्य रखा है।
उर्वरकों का असंतुलित प्रयोग
अनिवार्य वस्तु एक्ट, 1955 के तहत देश में उर्वरकों की मैन्यूफैक्चरिंग, बिक्री और वितरण को रसायन और उर्वरक मंत्रालय द्वारा रेगुलेट किया जाता है। उर्वरकों के तौर पर तीन मुख्य प्रकार के पोषक तत्वों का प्रयोग किया जाता है: नाइट्रोजन (एन), फॉस्फेट (पी), और पोटासिक (के)। इनमें से यूरिया (जिसमें एन उर्वरक होता है) की कीमत सरकार द्वारा नियंत्रित है, जबकि पी और के उर्वरकों को ज्वाइंट पार्लियामेंटरी कमिटी के सुझाव पर 1992 में नियंत्रण मुक्त कर दिया गया था। यह देखा गया है कि अन्य उर्वरकों की तुलना में यूरिया का उपयोग अधिक किया जाता है। हालांकि एनपीके उर्वरकों के प्रयोग का अनुशंसित अनुपात 4:2:1 है, भारत में यह अनुपात 6.7:2.4:1 है।6 पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में यूरिया का अत्यधिक उपयोग किया जाता है।6 रेखाचित्र 7 में पिछले दशक में उर्वरकों के उपयोग की प्रवृत्ति प्रदर्शित की गई है।
|
रेखाचित्र 7: उर्वरकों की खपत (लाख टन) स्रोत: एक नजर में कृषि सांख्यिकी 2015; पीआरएस। |
यूरिया के असंतुलित प्रयोग से एक समय के बाद मिट्टी का उपजाऊपन कम होता है और परिणामस्वरूप उत्पादकता पर असर होता है। देश में यूरिया (एन) सबसे अधिक उत्पादित (86%), उपभोग (74%) और आयात (52%) किया जाने वाला उर्वरक है।[49] सरकार ही यह तय करती है कि उर्वरकों को कितनी मात्रा में आयात किया जाए जोकि उनकी घरेलू उपलब्धता पर निर्भर करता है।
आयात की मात्रा को निर्धारित करने और आयातित उर्वरक को वास्तव में हासिल करने में 60-70 दिन लग जाते हैं, क्योंकि केवल तीन कंपनियों को देश में यूरिया आयात करने की अनुमति है। इसलिए यूरिया की बाजार में हमेशा कमी रहती है। चूंकि किसानों को यह सुनिश्चित करना होता है कि उनकी फसलों को समय पर यूरिया मिले, इसलिए कई बार यूरिया की बिक्री में काला बाजारी बढ़ जाती है और अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक की कीमत पर खरीद की जाती है।49
फसल के लिए उर्वरकों का अपेक्षित स्तर फसल के प्रकार पर निर्भर करता है। इसके अतिरिक्त यह इस बात पर निर्भर करता है कि मिट्टी का प्रकार क्या है, उपज का स्तर क्या है और पानी की उपलब्धता कितनी है।6 कुछ फसलों जैसे चावल, गेहूं, मक्का, कपास और गन्ने को दालों, फलों और सब्जियों की तुलना में अधिक मात्रा में नाइट्रोजन की जरूरत होती है। हालांकि विभिन्न फसलों में एन, पी और के उर्वरकों के प्रयोग का अनुपात बढ़ा है, अन्य देशों की तुलना में भारत में अब भी कम मात्रा में उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है। 2005-06 में उर्वरकों की औसत खपत 106 किलो प्रति हेक्टेयर थी, जो 2012-13 में बढ़कर 128 किलो प्रति हेक्टेयर हो गई। इसकी तुलना में पाकिस्तान में 205 किलो प्रति हेक्टेयर और चीन में 396 किलो प्रति हेक्टेयर उर्वरकों की खपत की जाती है।
|
पोषक तत्वों पर आधारित सबसिडी नीति केंद्र सरकार ने 2010 में पी और के उर्वरकों के लिए पोषक तत्वों पर आधारित सबसिडी नीति (एनबीएस) की शुरुआत की। एन, पी और के उर्वरकों के संतुलित प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए इस नीति को तैयार किया गया था। इस नीति के तहत पी और के उर्वरक बनाने वाली कंपनियों को यह छूट दी गई कि वे उचित स्तर पर अपने अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) को निर्धारित करें। सबसिडी पोषक तत्वों की प्रति किलो मात्रा के आधार पर दी जाएगी। इस नीति में उर्वरकों के देसी मैन्यूफैक्चरर को अतिरिक्त सबसिडी देने का भी प्रावधान है। एनबीसी नीति के प्रदर्शन पर भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि कार्यान्वयन के पांच वर्ष के बावजूद देश में उर्वरकों का प्रयोग संतुलित नहीं हुआ।[50] 2009-10 में जहां यूरिया के प्रयोग का अनुपात 4.3 था, वहीं 2012-13 में यह 8.2 हो गया। |
जैसा कि पहले कहा गया है, 2025 तक 300 मिलियन टन खाद्यान्न के उत्पादन के लक्ष्य को पूरा करने के लिए 45 मिलियन टन उर्वरकों की जरूरत होगी। इनमें से 6-7 मिलियन टन की जरूरत जैविक उर्वरकों से पूरी की जाएगी लेकिन बाकी बचा हिस्सा रासायनिक उर्वरकों से पूरा करना होगा (एन, पी और के उर्वरक)। इसके लिए उर्वरकों का घरेलू उत्पादन बढ़ाना होगा।6
उर्वरक सबसिडी
|
रेखाचित्र 8: उर्वरक सबसिडी (करोड़ रुपए में)
|
किसानों द्वारा उर्वरकों के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार उर्वरक निर्माताओं को सबसिडी देती है। 2017-18 में उर्वरक सबसिडी के लिए 70,000 करोड़ रुपए का आबंटन किया गया, जोकि खाद्य सबसिडी के बाद दूसरी सबसे बड़ी सबसिडी है।32 2000 से 2016 के बीच उर्वरक सबसिडी के लिए किए जाने वाले आबंटन में 11.4% की दर से वृद्धि हुई। 2016-17 की आबंटित सबसिडी में 49,768 करोड़ रुपए का आबंटन यूरिया के लिए किया गया। रेखाचित्र 8 में प्रदर्शित किया गया है कि 2000-01 के बाद से उर्वरक सबसिडी की क्या प्रवृत्ति रही है। |
वर्तमान में उर्वरक कंपनी की उत्पादन के लागत के आधार पर सबसिडी की राशि का निर्धारण किया जाता है।49 जिन कंपनियों के उत्पादन की लागत अधिक होती है, उन्हें सबसिडी मिलती है। इस वजह से कंपनियां उत्पादन की लागत को कम करने के बारे में नहीं सोचतीं। हालांकि पिछले दशक से यूरिया का उपयोग बढ़ा है, पिछले 15 वर्षों के दौरान घरेलू उत्पादन क्षमता में बढ़ोतरी नहीं हुई है।49
भारतीय खाद्य निगम की भूमिका की जांच करने वाली कमिटी ने सुझाव दिया था कि उर्वरक सबसिडी की मौजूदा प्रणाली के स्थान पर किसानों को नकद हस्तांतरण किए जाने चाहिए।[51] इससे वे अपनी जरूरत के अनुसार उर्वरकों को चुन सकेंगे और इससे मिट्टी में उर्वरकों के असंतुलन को दूर करने में मदद मिलेगी। केंद्रीय बजट 2016-17 में यह घोषणा की गई कि उर्वरकों के लिए प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण कार्यक्रम को देश के कुछ जिलों में पायलट आधार पर शुरू किया जाए।[52] जुलाई 2016 में सरकार ने घोषणा की कि 2016-17 के दौरान 16 जिलों में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरणों के लिए पायलट अध्ययन किए जाएंगे।[53]
कीटनाशकों का प्रयोग
देश में रासायनिक कीटनाशकों के उपभोग में पिछले कुछ वर्षों में बढ़ोतरी हुई है। 2010-11 में यह 55,540 टन से बढ़कर 2014-15 में 57,353 टन हो गया है।[54] इस अवधि के दौरान कीटनाशकों का आयात भी 53,996 टन से बढ़कर 77,376 टन हो गया है। कीटनाशकों से जुड़ी कुछ समस्याओं में उनका निम्न क्वालिटी का होना और उनके उपयोग के संबंध में जागरूकता का अभाव है। आर्थिक सर्वेक्षण 2015-16 में यह कहा गया था कि उचित दिशानिर्देशों के अभाव में कीटनाशकों का उपयोग करने के कारण भारत में खाद्य उत्पादों में कीटनाशकों के अवशेष पाए जाते हैं।18
कीटनाशकों के उत्पादन पर निगरानी रखने का काम रसायन और उर्वरक मंत्रालय का है, जबकि उसके उपयोग से जुड़े फैसले कृषि मंत्रालय द्वारा लिए जाते हैं। कीटनाशक क्षेत्र के लिए रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाने के लिए कीटनाशक एक्ट, 1968 की समीक्षा करने की जरूरत है।6कृषि संबंधी स्टैंडिंग कमिटी ने यह सुझाव भी दिया है कि देश में कीटनाशकों की मैन्यूफैक्चरिंग, आयात और बिक्री को रेगुलेट करने के लिए कीटनाशक विकास और रेगुलेशन अथॉरिटी बनाई जानी चाहिए।6इसके अतिरिक्त कमिटी ने एकीकृत कीट-प्रबंधन प्रणाली को विकसित करने, जिसमें कीट नियंत्रण के मैकेनिकल और बायोलॉजिकल तरीके दोनों शामिल हों, और जैविक कीटनाशकों के प्रयोग को बढ़ावा देने जैसे सुझाव भी दिए।18
अच्छी क्वालिटी के बीजों तक पहुंच
कृषि उत्पादकता को बढ़ाने के लिए अच्छी क्वालिटी के बीज दूसरी बड़ी जरूरत हैं। अच्छे बीज से कृषि उत्पादकता में 20% से 25% की वृद्धि होती है।[55] देश में बीज एक्ट, 1966 बीजों के रेगुलेशन का काम करता है। यह एक्ट बीजों की क्वालिटी, उत्पादन और बिक्री को रेगुलेट करता है। बीज नियंत्रण आदेश, 1983 बीजों को बेचने, निर्यात और आयात के लाइसेंसों को रेगुलेट करता है। बीजों की तीन किस्मों को सामान्य तौर पर प्रयोग किया जाता है। वे हैं : (i) खेती के दौरान बचाए गए बीज, जोकि कुल बीज उपभोग का 65% से 70% के करीब होते हैं, (ii) वाणिज्यिक स्तर पर उत्पादित बीजों की ब्रीडर, फाउंडेशन और सर्टिफाइड किस्में, और (iii) जेनिटिकली मॉडिफाइड और संकर (हाइब्रिड) बीज।
कृषि बीजों का उत्पादन विभिन्न एजेंसियों जैसे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और उसके अनुसंधान संस्थानों, राज्य कृषि विश्वविद्यालयों और राष्ट्रीय एवं राज्य बीज निगमों द्वारा किया जाता है। निजी क्षेत्र ने भी कुछ बीजों, जैसे हाइब्रिड मक्का, बाजरा, कपास और सूरजमुखी को सप्लाई करने में योगदान देना प्रारंभ किया है। अच्छी क्वालिटी के बीजों के विकास और वितरण में कुछ चुनौतियां भी हैं, जैसे (i) अच्छी क्वालिटी के बीजों की सुविधा, और (ii) अपर्याप्त अनुसंधान सहयोग।[56]
कुल उपलब्ध 30% से 35% बीजों का उत्पादन निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों द्वारा किया जाता है और बाकी के बीज खेतों में उत्पादित होने वाली फसलों से प्राप्त किए जाते हैं।18हालांकि किसान अपने खेतों की पैदावार से अनेक किस्म के बीज प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन उच्च उपज देने वाली किस्मों को बाजार से ही खरीदा जा सकता है। चूंकि इन किस्मों की कीमत अधिक होती है, इसलिए इन्हें चुकाना सीमांत और छोटे किसानों के लिए मुश्किल होता है। इससे वे इन बीजों को खरीदने के लिए हतोत्साहित होते हैं।43आर्थिक सर्वेक्षण 2015-16 में सुझाव दिया गया था कि बीज उत्पादन में अधिक कंपनियों को लाया जाना चाहिए जिससे बाजार में बीजों की उपलब्धता बढ़ेगी और उनकी कीमतों में गिरावट होगी।
|
जेनिटिकली मॉडिफाइड बीजों की किस्में जेनिटिकली मॉडिफाइड (जीएम) बीज ऐसे बीज होते हैं जिनके कुछ जीन्स को इस प्रकार बदला (मॉडिफाई किया) जाता है कि उनमें कीटों और हर्बिसाइड्स के प्रति प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो और उनकी उत्पादकता बढ़े। बीटी कॉटन भारत में एकमात्र स्वीकृत जीएम तकनीक वाले बीज हैं। 2002 में इसे अनुमोदित किया गया था और 2014 तक, कपास वाले 92% क्षेत्र में बीटी कॉटन का प्रयोग किया गया है।[57] देश में बीटी कॉटन का इस्तेमाल करने के बाद कपास की उपज 2000-01 में 190 किलो प्रति हेक्टेयर से बढ़कर 461 प्रति हेक्टेयर हो गई।[58] पिछले कुछ वर्षों के दौरान कई जीएम फसलों जैसे बीटी बैंगन को विकसित किया गया लेकिन उन्हें भारतीय बाजार में लाने को रेगुलेटरी मंजूरी नहीं मिली। वर्तमान रेगुलेटरी प्रक्रिया में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत आने वाली जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमिटी (जीईएसी) जीएम बीजों के वाणिज्यिक प्रयोग के प्रस्तावों को मंजूरी देती है।[59] सितंबर 2016 में जीईएसी ने जीई सरसों को पर्यावरणीय रूप से जारी करने को मंजूरी देने वाली एक रिपोर्ट पर आम जनता की प्रतिक्रियाएं आमंत्रित कीं।[60],[61]पर्यावरण मंत्रालय ने जीई सरसों को वाणिज्यिक रूप से जारी करने को अभी अंतिम मंजूरी नहीं दी है। |
कृषि मशीनरी
कृषि उत्पादकता पर मशीनीकरण का भी महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। कृषि मशीनरी का प्रयोग करने से खेतिहर मजदूरों को दूसरी गतिविधियों में लगाया जा सकता है। मशीनों का इस्तेमाल करने से जुताई, बीजों एवं उर्वरकों का छिड़काव और कटाई का काम ज्यादा अच्छी तरह से किया जा सकता है और इनपुट की लागत में भी कमी हो सकती है। इससे खेती का काम किफायती हो सकता है।
कृषि में मशीनीकरण की स्थिति भिन्न-भिन्न गतिविधियों में अलग-अलग है, हालांकि मशीनीकरण का समूचा स्तर विकसित देशों के मुकाबले काफी कम है। यहां 50% से भी कम मशीनों का इस्तेमाल होता है जबकि विकसित देशों में 90% के करीब।[62] मशीनीकरण का उच्चतम स्तर (60%-70%) कटाई, छंटाई की गतिविधियों और सिंचाई (37%) में पाया जाता है। मशीनों का सबसे कम इस्तेमाल बुवाई और रोपाई में किया जाता है। उत्पादकता बढ़ाने के लिए टिकाऊ, कम वजन और कम लागत वाले और विभिन्न फसलों एवं क्षेत्रों के अनुकूल उपकरणों को छोटे और सीमांत किसानों को उपलब्ध कराया जाना चाहिए।62
कृषि मशीनीकरण से जुड़ी चुनौतियों में भिन्न-भिन्न मिट्टी और जलवायु वाले क्षेत्र शामिल हैं जिनके लिए विशेष (कस्टमाइज) मशीनों की जरूरत होती है। साथ ही छोटी स्वामित्व वाली जमीनों के साथ संसाधनों तक सीमित पहुंच भी एक बड़ी समस्या है। मशीनीकरण का उद्देश्य यह होना चाहिए कि समय और श्रम की जरूरत कम पड़े, नुकसान कम से कम हो एवं श्रम की लागत में भी गिरावट आए, और इस प्रकार कार्यकुशलता बढ़ाई जाए।[63]
पैदावार के बाद की गतिविधियां
स्टोरेज की सुविधाएं
फसल की कटाई के बाद स्टोरेज के बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होती है ताकि मौसम की प्रतिकूल स्थिति और परिवहन के दौरान होने वाले नुकसान को कम से कम किया जा सके। कटाई और कटाई बाद की प्रक्रियाओं के दौरान खाद्यान्न का नुकसान पिछले पांच वर्षों में बढ़ा है।18सबसे अधिक नुकसान सब्जियों और फलों (2015 में उत्पादन का 4.6%-15.9%), दालों (6.4%-8.4%) और तिलहन (5.3%-9.9%) के मामलों में हुआ है।
खाद्यान्न का नुकसान खेती के सभी स्तरों पर होता है- किसान, ढुलाई करने वाला, थोक व्यापारी, खुदरा व्यापारी। इस नुकसान के कुछ कारण हैं, फसल बर्बाद होना, कटाई की अनुचित तकनीक, खराब पैकेजिंग और परिवहन, और खराब स्टोरेज। देश में स्टोरेज सुविधाओं की स्थिति से जुड़ी कुछ समस्याओं में स्टोरेज की अपर्याप्त क्षमता और खराब स्थितियां हैं।[64] जहां स्टोरेज क्षमता पर्याप्त है, वहां गोदाम उपयुक्त नहीं हैं। कहीं गोदाम नमी भरे हैं तो कहीं सुदूर जगह पर स्थित हैं।
केंद्रीय पूल के खाद्यान्नों को केंद्रीय भंडारण निगम (सीडब्ल्यूसी) के गोदामों रखा जाता है जोकि खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के तहत आता है। दिसंबर 2016 तक सीडब्ल्यूसी 9.7 मिलियन टन की कुल क्षमता वाले 438 गोदाम चला रहा था। राज्य भंडारण निगम राज्य स्तर पर गोदामों को प्रबंधित करते हैं। दिसंबर 2016 तक 19 निगम 26 मिलियन टन की कुल क्षमता वाले 1,757 गोदाम चला रहे थे।[65]
कृषि उत्पादों का स्टोरेज करने की एक प्रणाली और भी है जिसे सौदेबाजी करने लायक भंडारण प्रणाली कहा जाता है। वेयरहाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी (डब्ल्यूआरडीए) इसका रेगुलेशन करती है। इस प्रणाली के तहत उत्पादों को स्टोर करने वाले किसानों को एक रसीद जारी की जाती है जिसमें गोदाम की लोकेशन और स्टोर किए गए उत्पादों की गुणवत्ता और मात्रा का ब्यौरा होता है। अगर किसान कृषि ऋण प्राप्त करना चाहता है तो यह रसीद कोलेट्रल का काम करती है।[66] 2015 तक डब्ल्यूआरडीए के तहत पंजीकृत गोदामों की स्टोरेज क्षमता 118 मिलियन टन की थी। इसमें से 19 मिलियन टन निजी क्षेत्र और 15 मिलियन टन सहकारी क्षेत्र में आता था। बाकी का सरकारी स्टोरज के हिस्से था।[67]
चूंकि खाद्य पदार्थ, जैसे कुछ फल और सब्जियां जल्दी खराब होकर बर्बाद हो जाती हैं, इसलिए उन्हें नष्ट होने से बचाने के लिए ठंडे तापमान पर स्टोर करना पड़ता है।[68] देश में अनिवार्य वस्तु एक्ट, 1955 के तहत कोल्ड स्टोरेज आदेश, 1964 के माध्यम से कोल्ड स्टोरेज की सुविधाओं की शुरुआत की गई। देश में कोल्ड स्टोरेज के विकास की दिशा में कई चुनौतियां हैं, जैसे खेती की जमीन को औद्योगिक उपयोग के लिए इस्तेमाल करने के लिए भू-उपयोग में परिवर्तन करना पड़ता है और इस प्रक्रिया में विलंब होता है। इसके अतिरिक्त कृषि उत्पादों के कोल्ड स्टोरेज पर टैक्स छूट न मिलना, बिजली की पर्याप्त उपलब्धता न होना और किसानों की कोल्ड स्टोरेज तक पहुंच न होना भी समस्याएं पैदा करता है।[69]
|
मेगा फूड पार्क खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने 2008 में मेगा फूड पार्क योजना की शुरुआत की थी।[70] इस योजना का लक्ष्य कृषि उत्पादन को बाजार से जोड़ने वाले एक तंत्र का निर्माण करना है। इसमें क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण के साथ किसानों, प्रसंस्करण कंपनियों और रीटेलरों को शामिल किया जाता है। योजना के अपेक्षित परिणामों में किसानों को कृषि उत्पादों की उच्च कीमत, अच्छी क्वालिटी के खाद्य प्रसंस्करण इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थापना, खाद्य पदार्थों की बर्बादी का कम होना और कारगर खाद्य आपूर्ति श्रृंखला का सृजन इत्यादि शामिल है। कंपनी एक्ट, 2013 के तहत गठित स्पेशल पर्पज वेहिकल के जरिए इस योजना को लागू किया गया। जुलाई 2016 तक मंत्रालय ने 42 मेगा फूड पार्कों को मंजूरी दे दी थी, जिनमें से 38 को संचालित करने की मंजूरी मिल चुकी है। 8 मेगा फूड पार्क चल रहे हैं।[71] |
कृषि मूल्य
केंद्र या राज्य सरकारें कृषि उत्पादों की खरीद करती हैं। भारतीय खाद्य निगम कृषि उत्पादों की खरीद, स्टोरेज, मूवमेंट, वितरण और बिक्री का काम करता है।[72] न्यूनतम समर्थन मूल्य ऐसा मूल्य होता है, जिस पर सरकार किसानों से खाद्यान्न की खरीद करती है।
एमएसपी पर चावल और गेहूं की सबसे अधिक खरीद की जाती है। देश में पैदा होने वाले एक तिहाई गेहूं और चावल की खरीद केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। 2015-16 में देश में 33% गेहूं और 30% चावल की खरीद केंद्र सरकार द्वारा की गई थी। उल्लेखनीय है कि भारत गेहूं का बड़ा निर्यातक देश है। 2014-15 में देश में गेहूं का 90.8 मिलियन टन उत्पादन हुआ। इसमें से 28 मिलियन टन की खरीद केंद्रीय पूल के लिए की गई, जबकि 29 मिलियन टन का निर्यात किया गया।
न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी)
एमएसपी वह कीमत होती है, जिस पर केंद्र सरकार किसानों से खाद्यान्नों की खरीद करती है। किसानों को लाभकारी मूल्य प्राप्त हो, यह सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार एमएसपी का निर्धारण करती है। एमएसपी को निर्धारित करने के लिए जिन बातों पर विचार किया जाता है, उनमें पैदावार और उत्पादन की कीमत, फसल की उत्पादकता और बाजार मूल्य शामिल हैं।[73] फसल का अधिक एमएसपी मिलने पर किसानों को खेती की आधुनिक तकनीक और तौर-तरीकों को अपनाने के लिए प्रोत्साहन मिलता है। सरकार ने 22 फसलों के लिए एमएसपी (और चीनी के लिए उचित और लाभकारी मूल्य) की घोषणा की है लेकिन सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जिसके लिए खाद्यान्नों की खरीद की जाती है, मुख्य रूप से लाभार्थियों को गेहूं और चावल का वितरण ही करती है। चूंकि केवल गेहूं और चावल की ही खरीद की जाती है, इसलिए किसान दालों और तिलहन जैसी फसलों की बजाय इन्हीं फसलों की खेती करना पसंद करते हैं।37परिशिष्ट की तालिका 17 में 2005-06 से 2015-16 के बीच विभिन्न फसलों के लिए एमएसपी का विवरण दिया गया है।
एमएसपी का प्रभाव
हालांकि विभिन्न फसलों के लिए एमएसपी की घोषणा की जाती है, कुछ ही राज्यों में गेहूं, चावल, गन्ने और कपास की खरीद इन कीमतों पर की जाती है।[74] परिणामस्वरूप, सरकार की ओर से खरीद करने के कारण किसान दालों, तिलहन और मोटे अनाज की जगह इन फसलों की पैदावार पर अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं। बुवाई के हर मौसम (जून और अक्टूबर में) से पहले एमएसपी की घोषणा की जाती है, जिससे किसानों को यह जानकारी हो जाए कि सरकार उनके उत्पादों के लिए कितना न्यूनतम मूल्य देने वाली है। किसानों को फसल उत्पादन में निवेश बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु एमएसपी की घोषणा की जाती है।74एमएसपी के प्रभाव का आकलन करने के लिए नीति आयोग ने एक रिपोर्ट तैयार की जिसमें कहा गया है कि बुवाई के मौसम से पहले बहुत कम किसानों को एमएसपी की जानकारी होती है (10% को)। 62% किसानों को एमएसपी की जानकारी फसल की बुवाई के बाद होती है। एमएसपी की मूल्य नीति तब असरकारक होगी, जब किसानों को उस समय उसकी जानकारी हो, जब वे तय कर रहे हों कि उन्हें क्या फसल उगानी है। नीति आयोग ने सुझाव दिया कि एमएसपी के संबंध में किसानों की जागरूकता का स्तर बढ़ाया जाना चाहिए और इस सूचना को वितरित करने के माध्यमों को मजबूत किया जाना चाहिए।74
एमएसपी को लागू करने से संबंधित कई अन्य समस्याएं भी है, जैसे खरीद केंद्रों का दूर स्थित होना, किसानों के लिहाज से परिवहन की कीमत में बढ़ोतरी, खरीद केंद्रों का अनियमित समय, ढंके हुए गोदामों का कम होना और स्टोरेज की अपर्याप्त क्षमता, और किसानों को एमएसपी के भुगतान में होने वाला विलंब।74 नीति आयोग ने यह टिप्पणी की कि किसानों को अपने उत्पादों का लाभकारी मूल्य प्राप्त हो रहा है, यह सुनिश्चित करने के लिए कृषि मूल्य नीति की समीक्षा की जानी चाहिए। नीति आयोग ने प्राइस डेफिशिएंसी प्रणाली का सुझाव दिया। इस प्रणाली के तहत अगर मूल्यों में निश्चित सीमा से अधिक की गिरावट होती है तो किसानों को कुछ उत्पादों के लिए क्षतिपूर्ति की जाएगी। इससे किसानों की स्टॉक होल्डिंग में कमी आएगी, जो कीमतें बढ़ने के इंतजार में कृषि उत्पादों को स्टोर करके रखते हैं और किसानों को विभिन्न प्रकार की फसलों को उत्पादित करने के लिए बढ़ावा मिलेगा। किसानों को उनके आधार नंबर से लिंक्ड बैंक खातों के जरिए प्रत्यक्ष हस्तांतरण प्रणाली का प्रयोग करते हुए भुगतान किया जाएगा।
कृषि बाजार
कुछ वस्तुओं का उत्पादन, सप्लाई और वितरण अनिवार्य वस्तु एक्ट, 1955 के दायरे में आता है।[75] इन वस्तुओं में खाद्यान्न, तिलहन, सूती और ऊनी कपड़े, जूट और कोयला इत्यादि आते हैं। एक्ट के तहत केंद्र सरकार उस मूल्य को नियंत्रित कर सकती है, जिस पर किसी अनिवार्य वस्तु का व्यापार किया जाता है। सरकार उसके स्टोरेज, परिवहन, वितरण, निस्तारण या उपभोग के लाइसेंस को भी रेगुलेट कर सकती है।
देश में कृषि बाजारों को राज्य कृषि उत्पाद मार्केटिंग कमिटी (एपीएमसी) कानूनों द्वारा रेगुलेट किया जाता है।[76] इनके तहत किसानों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने कृषि उत्पादों को राज्य के स्वामित्व वाली मंडियों में बेचेंगे। पिछले कई वर्षों से इस प्रणाली में कई समस्याएं नजर आई हैं। उदाहरण के लिए वर्तमान में एपीएमसी मंडियां उन किसानों से एक मार्केट फी लेती हैं जो अपने कृषि उत्पाद बेचने वहां आते हैं। इससे किसानों के लिए एपीएमसी मंडियों में कृषि उत्पाद बेचना महंगा पड़ता है। इसके अतिरिक्त किसानों को कृषि उत्पादों को खेतों से पास की मंडी तक लाने की व्यवस्था करनी पड़ती है और उसके लिए परिवहन और ईंधन जैसे खर्चे करने पड़ते हैं। इन उत्पादों को खेतों से स्टोर तक लाने के दौरान बहुत से बिचौलिये शामिल होते हैं। इन बिचौलियों को उत्पाद की कीमत का एक अनुपात कमीशन के तौर पर चुकाया जाता है। इस प्रकार रीटेलर को अपना उत्पाद बेच कर किसान को जो कीमत मिलती है, उसकी तुलना में उसे मिलने वाला बाजार मूल्य काफी कम होता है।
केंद्र सरकार ने 2003 में मॉडल एपीएमसी एक्ट जारी किया जिसे राज्य द्वारा लागू किया जाना था।[77] मॉडल एक्ट में निम्नलिखित प्रावधान हैं : (i) कॉन्ट्रैक्ट खेती के जरिए उत्पादों की प्रत्यक्ष बिक्री, (ii) व्यक्तियों, किसानों और उपभोक्ताओं को कृषि बाजार स्थापित करने की अनुमति, (iii) कृषि उत्पादों की बिक्री पर सिंगल मार्केट फी की वसूली, और (iv) लाइसेंस को मार्केट एजेंसियों के पंजीकरण से बदलना, जिससे वे एक से अधिक बाजारों में ऑपरेट कर सकें, इत्यादि। हालांकि मॉडल एक्ट के सुधारों को केवल 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने ही लागू किया है।[78] चार राज्यों को इन सुधारों को अभी लागू करना है और बाकी के राज्य कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं।
आर्थिक सर्वेक्षण 2014-15 में किसानों को राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म देने के लिए राष्ट्रीय कृषि मार्केट (नैम) की स्थापना का सुझाव दिया गया जहां किसान अपने उत्पाद बेच सकते हैं।[79] ऐसे बाजार से किसान अपने कृषि उत्पादों को तदनुरूप मूल्य पर देश में कहीं भी बेच सकेंगे। अप्रैल 2016 में केंद्र सरकार ने 8 जिलों में राष्ट्रीय कृषि बाजार शुरू किए और एक कॉमन प्लेटफॉर्म बनाने के लिए इन क्षेत्रों में थोक मंडियों को एक दूसरे से जोड़ा। [80] एपीएमसी सुधारों को लागू करने से संबंधित राज्यों की स्थितियों की जानकारी परिशिष्ट की तालिका 18 में दी गई है।
परिशिष्ट
तालिका 6: 2010-11 के दौरान आकार के अनुसार राज्यों में भूमि स्वामित्व की संख्या (100 हेक्टेयर में)
|
राज्य |
सीमांत (<1 हेक्टेयर) |
छोटा (1-2 हेक्टेयर) |
मध्यम से कम (2-4 हेक्टेयर) |
मध्यम (4-10 हेक्टेयर) |
बड़ा (>10 हेक्टेयर) |
सभी स्वामित्व |
|
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह |
46 |
24 |
31 |
16 |
0 |
118 |
|
आंध्र प्रदेश |
84,247 |
29,184 |
13,991 |
3,973 |
357 |
1,31,751 |
|
अरुणाचल प्रदेश |
215 |
193 |
340 |
279 |
65 |
1,093 |
|
असम |
18,311 |
4,966 |
3,035 |
849 |
41 |
27,202 |
|
बिहार |
1,47,441 |
9,480 |
4,147 |
815 |
31 |
1,61,914 |
|
चंडीगढ़ |
5 |
1 |
1 |
0 |
0 |
7 |
|
छत्तीसगढ़ |
21,828 |
8,311 |
5,030 |
2,018 |
277 |
37,465 |
|
दादरा और नगर हवेली |
82 |
39 |
18 |
7 |
1 |
147 |
|
दमन और दीव |
77 |
5 |
1 |
0 |
0 |
84 |
|
दिल्ली |
113 |
45 |
30 |
15 |
2 |
205 |
|
गोवा |
599 |
98 |
57 |
20 |
6 |
780 |
|
गुजरात |
18,156 |
14,290 |
10,795 |
5,127 |
488 |
48,856 |
|
हरियाणा |
7,781 |
3,148 |
2,838 |
1,947 |
458 |
16,173 |
|
हिमाचल प्रदेश |
6,704 |
1,746 |
849 |
276 |
33 |
9,608 |
|
जम्मू और कश्मीर |
12,066 |
1,671 |
637 |
114 |
5 |
14,494 |
|
झारखंड |
18,483 |
4,289 |
2,828 |
1,287 |
202 |
27,089 |
|
कर्नाटक |
38,488 |
21,382 |
12,668 |
5,107 |
676 |
78,322 |
|
केरल |
65,797 |
1,802 |
570 |
120 |
19 |
68,308 |
|
लक्षदीप |
99 |
3 |
1 |
0 |
0 |
103 |
|
मध्य प्रदेश |
38,910 |
24,487 |
16,548 |
7,891 |
887 |
88,724 |
|
महाराष्ट्र |
67,090 |
40,523 |
21,591 |
7,106 |
679 |
1,36,990 |
|
मणिपुर |
767 |
222 |
28 |
0 |
1,506 |
- |
|
मेघालय |
1,027 |
578 |
405 |
83 |
2 |
2,096 |
|
मिजोरम |
502 |
298 |
99 |
17 |
3 |
919 |
|
नागालैंड |
65 |
203 |
485 |
780 |
252 |
1,784 |
|
ओड़िशा |
33,683 |
9,186 |
3,113 |
637 |
56 |
46,675 |
|
पुद्दूचेरी |
285 |
28 |
14 |
4 |
1 |
332 |
|
पंजाब |
1,644 |
1,954 |
3,245 |
2,985 |
697 |
10,526 |
|
राजस्थान |
25,115 |
15,111 |
13,351 |
11,271 |
4,036 |
68,884 |
|
सिक्किम |
405 |
169 |
108 |
59 |
8 |
749 |
|
तमिलनाडु |
62,666 |
11,813 |
5,023 |
1,506 |
174 |
81,182 |
|
त्रिपुरा |
4,991 |
550 |
215 |
28 |
1 |
5,785 |
|
उत्तर प्रदेश |
1,85,323 |
30,353 |
13,343 |
3,983 |
253 |
2,33,255 |
|
उत्तराखंड |
6,721 |
1,573 |
648 |
173 |
11 |
9,127 |
|
पश्चिम बंगाल |
58,527 |
9,798 |
2,675 |
227 |
7 |
71,233 |
|
कुल |
9,28,260 |
2,47,792 |
1,38,956 |
58,750 |
9,728 |
13,83,485 |
स्रोत: तालिका 15.2 (क) एक नजर में कृषि सांख्यिकी, 2015, कृषि मंत्रालय; पीआरएस।
तालिका 7: फसलों का उत्पादन (मिलियन टन में)
|
वर्ष |
चावल |
गेहूं |
मोटे अनाज |
दालें |
कुल खाद्यान्न |
तिलहन |
कपास |
चीनी |
|
1950-51 |
21 |
6 |
15 |
8 |
51 |
5 |
3 |
57 |
|
1960-61 |
35 |
11 |
24 |
13 |
82 |
7 |
6 |
110 |
|
1970-71 |
42 |
24 |
31 |
12 |
108 |
10 |
5 |
126 |
|
1980-81 |
54 |
36 |
29 |
11 |
130 |
9 |
7 |
154 |
|
1990-91 |
74 |
55 |
33 |
14 |
176 |
19 |
10 |
241 |
|
2000-01 |
85 |
70 |
31 |
11 |
197 |
18 |
10 |
296 |
|
2010-11 |
96 |
87 |
43 |
18 |
244 |
32 |
33 |
342 |
|
2014-15 |
105 |
87 |
43 |
17 |
252 |
28 |
35 |
362 |
|
2015-16 |
104 |
94 |
38 |
16 |
252 |
25 |
30 |
352 |
नोट: कपास उत्पादन 170 किलोग्राम प्रति गांठ में है।
स्रोत: एक नजर में कृषि सांख्यिकी, 2015, कृषि मंत्रालय; पीआरएस।
तालिका 8: 2014-15 के दौरान मुख्य फसलों की पैदावार करने वाले प्रमुख राज्य
|
राज्य |
उत्पादन (मिलियन टन) |
पूरे भारत में % |
उपज (किलो प्रति हेक्टेयर) |
सिंचाई के तहत क्षेत्र (%) |
|
चावल |
||||
|
पश्चिम बंगाल |
14.7 |
14.0 |
2,731 |
48.2% |
|
उत्तर प्रदेश |
12.2 |
11.7 |
2,082 |
83.1% |
|
आंध्र प्रदेश |
11.6 |
11.0 |
3,036 |
96.8% |
|
भारत |
104.8 |
2,390 |
58.3% |
|
|
गेहूं |
||||
|
उत्तर प्रदेश |
25.2 |
28.4 |
2,561 |
98.4% |
|
पंजाब |
15.8 |
17.7 |
4,491 |
98.9% |
|
मध्य प्रदेश |
14.2 |
16.0 |
2,551 |
90.8% |
|
भारत |
88.9 |
2,872 |
93.4% |
|
|
मक्का |
||||
|
आंध्र प्रदेश |
4.2 |
17.9 |
4,257 |
49.5% |
|
कर्नाटक |
3.9 |
16.5 |
2,921 |
36.0% |
|
महाराष्ट्र |
2.2 |
9.3 |
2,080 |
12.7% |
|
भारत |
23.7 |
2,557 |
25.4% |
|
|
मोटे अनाज |
||||
|
राजस्थान |
7.6 |
18.1 |
1,257 |
7.4% |
|
कर्नाटक |
6.7 |
16.0 |
1,992 |
20.1% |
|
आंध्र प्रदेश |
4.7 |
11.3 |
3,596 |
39.7% |
|
भारत |
41.8 |
1,729 |
16.5% |
|
|
दालें |
||||
|
मध्य प्रदेश |
4.7 |
27.4 |
877 |
38.5% |
|
राजस्थान |
2.0 |
11.3 |
580 |
21.1% |
|
महाराष्ट्र |
1.7 |
10.1 |
553 |
9.2% |
|
भारत |
17.2 |
744 |
18.6% |
|
|
तिलहन |
||||
|
मध्य प्रदेश |
7.7 |
29.0 |
1,090 |
5.5% |
|
राजस्थान |
5.3 |
20.0 |
1,192 |
60.4% |
|
गुजरात |
4.0 |
14.9 |
1,550 |
31.3% |
|
भारत |
26.7 |
1,037 |
28.3% |
|
|
चीनी |
||||
|
उत्तर प्रदेश |
138.5 |
38.5 |
62,154 |
95.1% |
|
महाराष्ट्र |
81.9 |
22.8 |
78,120 |
100.0% |
|
कर्नाटक |
41.9 |
11.7 |
93,100 |
100.0% |
|
भारत |
359.3 |
69,860 |
95.0% |
|
|
कपास, (मिलियन गांठ में : 1 गांठ = 170 किलोग्राम) |
||||
|
गुजरात |
11.1 |
31.3 |
626 |
58.7% |
|
महाराष्ट्र |
7.0 |
19.8 |
285 |
2.7% |
|
आंध्र प्रदेश |
6.6 |
18.7 |
444 |
13.9% |
|
भारत |
35.5 |
461 |
33.8% |
|
स्रोत: एक नजर में कृषि सांख्यिकी, 2015, कृषि मंत्रालय; पीआरएस।
तालिका 9: खाद्यान्नों की राज्य वार उपज (किलो प्रति हेक्टेयर में)
|
राज्य/केंद्र शासित प्रदेश |
2004-05 |
2005-06 |
2006-07 |
2007-08 |
2008-09 |
2009-10 |
2010-11 |
2011-12 |
2012-13 |
2013-14 |
2014-15* |
|
आंध्र प्रदेश |
2,138 |
2,365 |
2,231 |
2,613 |
2,744 |
2,294 |
2,530 |
2,519 |
2,670 |
2,661 |
2,653 |
|
अरुणाचल प्रदेश |
1,178 |
1,212 |
1,216 |
1,241 |
1,255 |
1,555 |
1,673 |
1,778 |
1,786 |
1,794 |
# |
|
असम |
1,405 |
1,416 |
1,286 |
1,378 |
1,551 |
1,662 |
1,763 |
1,704 |
1,962 |
1,916 |
2,012 |
|
बिहार |
1,192 |
1,311 |
1,656 |
1,546 |
1,766 |
1,530 |
1,479 |
2,098 |
2,366 |
2,018 |
1,948 |
|
छत्तीसगढ़ |
979 |
1,111 |
1,148 |
1,238 |
1,041 |
1,008 |
1,424 |
1,384 |
1,506 |
1,524 |
1,433 |
|
गोवा |
2,456 |
2,509 |
2,254 |
2,091 |
2,231 |
1,990 |
2,264 |
2,272 |
2,361 |
2,659 |
# |
|
गुजरात |
1,412 |
1,551 |
1,423 |
1,831 |
1,595 |
1,560 |
1,843 |
1,874 |
1,970 |
2,097 |
1,955 |
|
हरियाणा |
3,092 |
3,045 |
3,393 |
3,420 |
3,388 |
3,383 |
3,526 |
3,879 |
3,689 |
3,855 |
3,772 |
|
हिमाचल प्रदेश |
1,923 |
1,731 |
1,714 |
1,918 |
1,757 |
1,297 |
1,787 |
1,911 |
1,850 |
1,962 |
2,011 |
|
जम्मू और कश्मीर |
1,686 |
1,680 |
1,733 |
1,711 |
1,851 |
1,405 |
1,639 |
1,690 |
1,962 |
1,915 |
1,379 |
|
झारखंड |
1,234 |
1,073 |
1,550 |
1,709 |
1,720 |
1,330 |
1,257 |
1,798 |
1,876 |
1,891 |
1,855 |
|
कर्नाटक |
1,388 |
1,776 |
1,289 |
1,548 |
1,511 |
1,377 |
1,684 |
1,629 |
1,488 |
1,620 |
1,684 |
|
केरल |
2,278 |
2,219 |
2,331 |
2,221 |
2,440 |
2,470 |
2,399 |
2,695 |
2,547 |
2,530 |
2,805 |
|
मध्य प्रदेश |
1,131 |
1,130 |
1,167 |
1,069 |
1,168 |
1,285 |
1,162 |
1,510 |
1,676 |
1,603 |
1,719 |
|
महाराष्ट्र |
836 |
948 |
940 |
1,150 |
1,001 |
1,039 |
1,184 |
1,155 |
1,038 |
1,207 |
1,043 |
|
मणिपुर |
2,390 |
2,241 |
2,241 |
2,297 |
2,236 |
1,796 |
2,244 |
2,397 |
1,926 |
1,745 |
# |
|
मेघालय |
1,674 |
1,455 |
1,800 |
1,774 |
1,783 |
1,809 |
1,803 |
1,873 |
1,997 |
2,387 |
# |
|
मिजोरम |
1,888 |
1,754 |
822 |
285 |
898 |
1,047 |
1,246 |
1,382 |
1,756 |
1,506 |
# |
|
नागालैंड |
1,577 |
1,615 |
1,482 |
1,567 |
1,811 |
1,256 |
1,958 |
1,967 |
2,027 |
2,018 |
# |
|
ओड़िशा |
1,300 |
1,349 |
1,369 |
1,484 |
1,363 |
1,262 |
1,432 |
1,303 |
1,592 |
1,625 |
1,733 |
|
पंजाब |
4,040 |
3,986 |
1,359 |
4,255 |
4,231 |
4,144 |
4,280 |
4,364 |
4,347 |
4,500 |
4,144 |
|
राजस्थान |
1,008 |
919 |
4,017 |
1,180 |
1,263 |
931 |
1,249 |
1,348 |
1,480 |
1,334 |
1,535 |
|
सिक्किम |
1,406 |
1,354 |
991 |
1,378 |
1,351 |
1,496 |
1,448 |
1,495 |
1,608 |
1,577 |
# |
|
तमिलनाडु |
1,874 |
1,847 |
1,354 |
2,125 |
2,225 |
2,477 |
2,393 |
3,162 |
2,131 |
2,554 |
2,529 |
|
त्रिपुरा |
2,179 |
2,194 |
2,610 |
2,563 |
2,526 |
2,544 |
2,587 |
2,620 |
2,711 |
2,680 |
# |
|
उत्तर प्रदेश |
1,961 |
2,057 |
2,399 |
2,206 |
2,365 |
2,236 |
2,386 |
2,498 |
2,542 |
2,484 |
2,117 |
|
उत्तराखंड |
1,697 |
1,548 |
2,057 |
1,785 |
1,715 |
1,780 |
1,841 |
1,945 |
1,962 |
1,995 |
1,824 |
|
पश्चिम बंगाल |
2,479 |
2,423 |
1,760 |
2,525 |
2,493 |
2,522 |
2,601 |
2,645 |
2,717 |
2,721 |
2,691 |
|
अन्य |
उपलब्ध नहीं |
उपलब्ध नहीं |
उपलब्ध नहीं |
उपलब्ध नहीं |
उपलब्ध नहीं |
उपलब्ध नहीं |
उपलब्ध नहीं |
उपलब्ध नहीं |
उपलब्ध नहीं |
उपलब्ध नहीं |
2,778 |
|
भारत |
1,652 |
1,715 |
1,756 |
1,860 |
1,909 |
1,798 |
1,930 |
2,078 |
2,129 |
2,120 |
2,070 |
* चौथे अग्रिम अनुमान
स्रोत: एक नजर में कृषि सांख्यिकी, 2015, कृषि मंत्रालय; पीआरएस।
तालिका 10: गेहूं की राज्य वार उपज (किलो प्रति हेक्टेयर में)
|
राज्य/केंद्र शासित प्रदेश |
2005-06 |
2006-07 |
2007-08 |
2008-09 |
2009-10 |
2010-11 |
2011-12 |
2012-13 |
2013-14 |
2014-15 |
|
आंध्र प्रदेश |
818 |
900 |
889 |
1,143 |
1,000 |
1,300 |
1,375 |
1,250 |
500 |
1,000 |
|
अरुणाचल प्रदेश |
1,525 |
1,575 |
1,472 |
1,576 |
1,505 |
1,595 |
1,757 |
1,498 |
1,510 |
* |
|
असम |
1,074 |
1,117 |
1,268 |
1,090 |
1,087 |
1,179 |
1,147 |
1,304 |
1,292 |
1,257 |
|
बिहार |
1,617 |
1,908 |
2,058 |
2,043 |
2,084 |
1,948 |
2,206 |
2,427 |
2,358 |
1,851 |
|
छत्तीसगढ़ |
886 |
1,002 |
1,059 |
1,040 |
1,086 |
1,144 |
1,227 |
1,396 |
1,304 |
1,388 |
|
गुजरात |
2,700 |
2,498 |
3,013 |
2,377 |
2,679 |
3,155 |
3,014 |
2,875 |
3,255 |
2,810 |
|
हरियाणा |
3,844 |
4,232 |
4,158 |
4,390 |
4,213 |
4,624 |
5,030 |
4,452 |
4,722 |
4,574 |
|
हिमाचल प्रदेश |
1,894 |
1,385 |
1,376 |
1,520 |
928 |
1,530 |
1,671 |
1,671 |
1,873 |
1,800 |
|
जम्मू और कश्मीर |
1,790 |
1,893 |
1,782 |
1,735 |
1,003 |
1,535 |
1,689 |
1,595 |
2,061 |
1,200 |
|
झारखंड |
1,340 |
1,529 |
1,621 |
1,541 |
1,738 |
1,642 |
1,908 |
1,944 |
2,123 |
1,931 |
|
कर्नाटक |
858 |
762 |
946 |
918 |
887 |
1,094 |
858 |
796 |
1,005 |
1,091 |
|
मध्य प्रदेश |
1,613 |
1,835 |
1,612 |
1,723 |
1,967 |
1,757 |
2,360 |
2,478 |
2,405 |
2,551 |
|
महाराष्ट्र |
1,393 |
1,325 |
1,659 |
1,483 |
1,610 |
1,761 |
1,558 |
1,528 |
1,460 |
1,381 |
|
मेघालय |
1,714 |
2,000 |
1,833 |
1,750 |
1,773 |
1,791 |
1,564 |
1,806 |
1,881 |
* |
|
नागालैंड |
1,583 |
867 |
1,067 |
1,500 |
1,200 |
1,712 |
1,711 |
1,801 |
1,823 |
* |
|
ओड़िशा |
1,364 |
1,487 |
1,554 |
1,396 |
1,450 |
1,458 |
1,644 |
1,894 |
1,574 |
1,772 |
|
पंजाब |
4,179 |
4,210 |
4,507 |
4,462 |
4,307 |
4,693 |
4,898 |
4,724 |
5,017 |
4,492 |
|
राजस्थान |
2,762 |
2,751 |
2,749 |
3,175 |
3,133 |
2,910 |
3,175 |
3,028 |
3,083 |
2,974 |
|
सिक्किम |
1,385 |
1,385 |
1,000 |
1,345 |
1,135 |
1,023 |
1,060 |
1,058 |
1,083 |
* |
|
त्रिपुरा |
2,636 |
1,800 |
1,900 |
2,000 |
1,984 |
2,025 |
2,000 |
2,000 |
2,000 |
* |
|
उत्तर प्रदेश |
2,627 |
2,721 |
2,817 |
3,002 |
2,846 |
3,113 |
3,113 |
3,113 |
3,038 |
2,561 |
|
उत्तराखंड |
1,633 |
2,049 |
2,050 |
2,003 |
2,139 |
2,316 |
2,379 |
2,396 |
2,422 |
1,902 |
|
पश्चिम बंगाल |
2,109 |
2,282 |
2,602 |
2,490 |
2,680 |
2,760 |
2,765 |
2,786 |
2,791 |
2,836 |
|
भारत |
2,619 |
2,708 |
2,802 |
2,907 |
2,839 |
2,989 |
3,177 |
3,117 |
3,145 |
2,872 |
नोट : 2014-15 के आंकड़े चौथे अग्रिम अनुमान हैं। *2014-15 में अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा की उपज जुड़कर 3,902 किलो प्रति हेक्टेयर होती है।
स्रोत: एक नजर में कृषि सांख्यिकी, 2015, कृषि मंत्रालय; पीआरएस।
तालिका 11: चावल की राज्य वार उपज (किलो प्रति हेक्टेयर में)
|
राज्य/केंद्र शासित प्रदेश |
2005-06 |
2006-07 |
2007-08 |
2008-09 |
2009-10 |
2010-11 |
2011-12 |
2012-13 |
2013-14 |
2014-15 |
|
आंध्र प्रदेश |
2,939 |
2,984 |
3,344 |
3,246 |
3,062 |
3,035 |
3,148 |
3,173 |
2,921 |
3,036 |
|
अरुणाचल प्रदेश |
1,195 |
1,195 |
1,275 |
1,293 |
1,777 |
1,925 |
2,065 |
2,086 |
2,092 |
* |
|
असम |
1,468 |
1,332 |
1,428 |
1,614 |
1,737 |
1,843 |
1,780 |
2,061 |
2,012 |
2,135 |
|
बिहार |
1,075 |
1,486 |
1,237 |
1,599 |
1,120 |
1,095 |
2,155 |
2,282 |
1,759 |
1,951 |
|
छत्तीसगढ़ |
1,337 |
1,354 |
1,446 |
1,176 |
1,120 |
1,663 |
1,597 |
1,746 |
1,766 |
1,581 |
|
गोवा |
2,822 |
2,458 |
2,330 |
2,466 |
2,136 |
2,467 |
2,577 |
2,679 |
2,954 |
* |
|
गुजरात |
1,949 |
1,894 |
1,942 |
1,744 |
1,903 |
1,852 |
2,141 |
2,198 |
2,076 |
2,085 |
|
हरियाणा |
3,051 |
3,238 |
3,361 |
2,726 |
3,008 |
2,789 |
3,044 |
3,272 |
3,256 |
3,113 |
|
हिमाचल प्रदेश |
1,412 |
1,559 |
1,546 |
1,523 |
1,381 |
1,673 |
1,705 |
1,629 |
1,625 |
1,751 |
|
जम्मू और कश्मीर |
2,150 |
2,194 |
2,133 |
2,186 |
1,914 |
1,942 |
2,078 |
3,126 |
2,250 |
1,710 |
|
झारखंड |
1,150 |
1,828 |
2,018 |
2,031 |
1,546 |
1,541 |
2,131 |
2,238 |
2,238 |
2,210 |
|
कर्नाटक |
3,868 |
2,470 |
2,625 |
2,511 |
2,482 |
2,719 |
2,793 |
2,632 |
2,666 |
2,827 |
|
केरल |
2,284 |
2,390 |
2,310 |
2,519 |
2,557 |
2,452 |
2,733 |
2,577 |
2,551 |
2,818 |
|
मध्य प्रदेश |
999 |
824 |
938 |
927 |
872 |
1,106 |
1,340 |
1,474 |
1,474 |
1,684 |
|
महाराष्ट्र |
1,770 |
1,669 |
1,898 |
1,489 |
1,474 |
1,766 |
1,837 |
1,965 |
1,924 |
1,891 |
|
मणिपुर |
2,322 |
2,322 |
2,446 |
2,357 |
1,889 |
2,453 |
2,642 |
2,546 |
2,201 |
* |
|
मेघालय |
1,508 |
1,916 |
1,880 |
1,886 |
1,910 |
1,912 |
1,988 |
2,125 |
2,493 |
* |
|
मिजोरम |
1,778 |
559 |
288 |
885 |
939 |
1,160 |
1,411 |
2,088 |
1,522 |
* |
|
नागालैंड |
1,682 |
1,600 |
1,685 |
1,994 |
1,426 |
2,102 |
2,106 |
2,204 |
2,260 |
* |
|
ओड़िशा |
1,531 |
1,534 |
1,694 |
1,529 |
1,585 |
1,616 |
1,450 |
1,814 |
1,821 |
1,989 |
|
पंजाब |
3,858 |
3,868 |
4,019 |
4,022 |
4,010 |
3,828 |
3,741 |
3,998 |
3,952 |
3,838 |
|
राजस्थान |
1,425 |
1,577 |
2,031 |
1,807 |
1,515 |
2,025 |
1,886 |
1,771 |
2,147 |
2,186 |
|
सिक्किम |
1,433 |
1,433 |
1,636 |
1,476 |
1,869 |
1,727 |
1,730 |
1,790 |
1,815 |
* |
|
तमिलनाडु |
2,546 |
3,423 |
2,817 |
2,683 |
3,070 |
3,040 |
3,918 |
2,772 |
3,100 |
3,191 |
|
त्रिपुरा |
2,260 |
2,472 |
2,633 |
2,586 |
2,606 |
2,655 |
2,700 |
2,800 |
2,800 |
* |
|
उत्तर प्रदेश |
1,996 |
1,879 |
2,063 |
2,171 |
2,084 |
2,120 |
2,358 |
2,460 |
2,447 |
2,082 |
|
उत्तराखंड |
1,954 |
1,979 |
2,052 |
1,966 |
2,068 |
1,901 |
2,121 |
2,206 |
2,289 |
2,313 |
|
पश्चिम बंगाल |
2,509 |
2,593 |
2,573 |
2,533 |
2,547 |
2,639 |
2,688 |
2,760 |
2,788 |
2,731 |
|
भारत |
2,102 |
2,131 |
2,202 |
2,178 |
2,125 |
2,239 |
2,393 |
2,461 |
2,416 |
2,390 |
नोट : 2014-15 के आंकड़े चौथे अग्रिम अनुमान हैं। *2014-15 में अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा की उपज जुड़कर 2,488 किलो प्रति हेक्टेयर होती है।
स्रोत: एक नजर में कृषि सांख्यिकी, 2015; पीआरएस।
तालिका 12: दालों की राज्य वार उपज (किलो प्रति हेक्टेयर में)
|
राज्य/केंद्र शासित प्रदेश |
2005-06 |
2006-07 |
2007-08 |
2008-09 |
2009-10 |
2010-11 |
2011-12 |
2012-13 |
2013-14 |
2014-15 |
|
आंध्र प्रदेश |
772 |
679 |
803 |
818 |
740 |
675 |
637 |
833 |
928 |
797 |
|
अरुणाचल प्रदेश |
1,078 |
1,078 |
1,078 |
1,059 |
1,000 |
879 |
920 |
1,076 |
1,149 |
* |
|
असम |
537 |
557 |
558 |
567 |
560 |
555 |
573 |
598 |
695 |
642 |
|
बिहार |
749 |
722 |
818 |
801 |
836 |
878 |
975 |
1,052 |
1,044 |
830 |
|
छत्तीसगढ़ |
477 |
543 |
586 |
580 |
604 |
624 |
613 |
700 |
574 |
834 |
|
गोवा |
1,045 |
1,358 |
991 |
1,030 |
1,082 |
1,057 |
836 |
902 |
1,102 |
* |
|
गुजरात |
704 |
593 |
843 |
777 |
705 |
812 |
815 |
867 |
897 |
912 |
|
हरियाणा |
622 |
824 |
602 |
972 |
758 |
899 |
706 |
800 |
819 |
692 |
|
हिमाचल प्रदेश |
713 |
932 |
1,062 |
758 |
681 |
1,213 |
954 |
1,413 |
1,763 |
1,251 |
|
जम्मू और कश्मीर |
504 |
505 |
508 |
464 |
456 |
584 |
508 |
530 |
535 |
292 |
|
झारखंड |
567 |
686 |
736 |
724 |
709 |
773 |
885 |
1,038 |
1,021 |
1,004 |
|
कर्नाटक |
487 |
377 |
531 |
466 |
451 |
561 |
492 |
555 |
641 |
644 |
|
केरल |
775 |
857 |
857 |
818 |
991 |
778 |
747 |
1,042 |
1,091 |
1,158 |
|
मध्य प्रदेश |
754 |
780 |
609 |
808 |
871 |
656 |
803 |
972 |
861 |
877 |
|
महाराष्ट्र |
584 |
602 |
746 |
537 |
702 |
768 |
693 |
704 |
802 |
554 |
|
मणिपुर |
523 |
523 |
497 |
504 |
497 |
897 |
942 |
936 |
933 |
* |
|
मेघालय |
750 |
744 |
825 |
867 |
881 |
881 |
896 |
1,019 |
1,092 |
* |
|
मिजोरम |
1,215 |
1,160 |
529 |
900 |
1,667 |
1,534 |
1,389 |
1,061 |
1,468 |
* |
|
नागालैंड |
1,281 |
1,200 |
1,189 |
1,203 |
906 |
1,085 |
1,091 |
1,099 |
1,124 |
* |
|
ओड़िशा |
416 |
445 |
446 |
481 |
461 |
486 |
471 |
513 |
537 |
527 |
|
पंजाब |
804 |
850 |
804 |
908 |
896 |
910 |
789 |
823 |
872 |
894 |
|
राजस्थान |
261 |
462 |
401 |
497 |
204 |
685 |
546 |
603 |
593 |
580 |
|
सिक्किम |
897 |
897 |
928 |
937 |
977 |
899 |
903 |
915 |
925 |
* |
|
तमिलनाडु |
337 |
541 |
303 |
307 |
382 |
386 |
552 |
413 |
752 |
689 |
|
त्रिपुरा |
629 |
654 |
691 |
718 |
713 |
706 |
697 |
705 |
719 |
* |
|
उत्तर प्रदेश |
811 |
725 |
731 |
899 |
748 |
832 |
993 |
985 |
736 |
618 |
|
उत्तराखंड |
590 |
642 |
794 |
609 |
719 |
851 |
891 |
841 |
869 |
799 |
|
पश्चिम बंगाल |
785 |
703 |
793 |
704 |
826 |
898 |
706 |
952 |
843 |
713 |
|
भारत |
598 |
612 |
625 |
659 |
630 |
691 |
699 |
789 |
764 |
744 |
नोट : 2014-15 के आंकड़े चौथे अग्रिम अनुमान हैं। *2014-15 में अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा की उपज जुड़कर 7,029 किलो प्रति हेक्टेयर होती है।
स्रोत: एक नजर में कृषि सांख्यिकी, 2015; पीआरएस।
तालिका 13: तिलहन की राज्य वार उपज (किलो प्रति हेक्टेयर में)
|
राज्य/केंद्र शासित प्रदेश |
2005-06 |
2006-07 |
2007-08 |
2008-09 |
2009-10 |
2010-11 |
2011-12 |
2012-13 |
2013-14 |
2014-15 |
|
आंध्र प्रदेश |
698 |
609 |
1,276 |
842 |
724 |
861 |
650 |
849 |
929 |
778 |
|
अरुणाचल प्रदेश |
838 |
838 |
962 |
963 |
928 |
921 |
1,015 |
909 |
958 |
* |
|
असम |
465 |
495 |
523 |
542 |
526 |
576 |
557 |
610 |
611 |
628 |
|
बिहार |
982 |
1,031 |
979 |
999 |
1,042 |
1,048 |
1,046 |
1,120 |
1,189 |
1,058 |
|
छत्तीसगढ़ |
419 |
503 |
532 |
507 |
607 |
686 |
550 |
723 |
640 |
595 |
|
गोवा |
2,394 |
1,769 |
1,892 |
2,158 |
2,807 |
2,862 |
2,500 |
2,409 |
2,544 |
* |
|
गुजरात |
1,544 |
908 |
1,618 |
1,345 |
1,109 |
1,692 |
1,608 |
1,103 |
2,231 |
1,551 |
|
हरियाणा |
1,124 |
1,344 |
1,214 |
1,723 |
1,645 |
1,855 |
1,394 |
1,712 |
1,637 |
1,415 |
|
हिमाचल प्रदेश |
344 |
477 |
442 |
365 |
271 |
514 |
579 |
514 |
490 |
591 |
|
जम्मू और कश्मीर |
429 |
610 |
846 |
760 |
763 |
821 |
826 |
789 |
895 |
670 |
|
झारखंड |
311 |
422 |
553 |
560 |
563 |
625 |
680 |
787 |
663 |
652 |
|
कर्नाटक |
600 |
478 |
681 |
556 |
502 |
782 |
665 |
647 |
824 |
773 |
|
केरल |
667 |
889 |
706 |
696 |
632 |
1,032 |
1,230 |
1,045 |
980 |
1,179 |
|
मध्य प्रदेश |
1,009 |
955 |
1,015 |
1,075 |
1,129 |
1,143 |
1,073 |
1,231 |
858 |
1,090 |
|
महाराष्ट्र |
925 |
963 |
1,274 |
857 |
725 |
1,394 |
1,223 |
1,337 |
1,276 |
658 |
|
मणिपुर |
7,000 |
7,000 |
उपलब्ध नहीं |
778 |
778 |
774 |
788 |
729 |
840 |
* |
|
मेघालय |
684 |
673 |
670 |
676 |
701 |
704 |
766 |
695 |
1,030 |
* |
|
मिजोरम |
1,125 |
927 |
229 |
781 |
1,106 |
1,203 |
967 |
1,078 |
1,146 |
* |
|
नागालैंड |
926 |
901 |
896 |
1,142 |
835 |
1,040 |
1,043 |
1,047 |
1,048 |
* |
|
ओड़िशा |
565 |
550 |
608 |
604 |
589 |
619 |
661 |
700 |
755 |
692 |
|
पंजाब |
1,097 |
1,111 |
1,288 |
1,276 |
1,354 |
1,336 |
1,360 |
1,350 |
1,335 |
1,065 |
|
राजस्थान |
1,134 |
1,146 |
1,051 |
1,114 |
1,066 |
1,203 |
1,243 |
1,296 |
1,144 |
1,192 |
|
सिक्किम |
727 |
727 |
872 |
763 |
959 |
832 |
841 |
863 |
887 |
* |
|
तमिलनाडु |
1,624 |
1,829 |
1,739 |
1,782 |
1,898 |
2,077 |
2,479 |
2,103 |
2,362 |
2,292 |
|
त्रिपुरा |
709 |
705 |
675 |
714 |
717 |
732 |
751 |
506 |
759 |
* |
|
उत्तर प्रदेश |
857 |
993 |
837 |
856 |
865 |
753 |
832 |
828 |
898 |
699 |
|
उत्तराखंड |
750 |
967 |
1,000 |
1,138 |
1,012 |
1,082 |
1,236 |
1,070 |
892 |
892 |
|
पश्चिम बंगाल |
952 |
918 |
997 |
828 |
1,065 |
1,047 |
994 |
1,162 |
1,181 |
1,194 |
|
भारत |
1,004 |
916 |
1,115 |
1,006 |
958 |
1,193 |
1,133 |
1,168 |
1,168 |
1,037 |
नोट : 2014-15 के आंकड़े चौथे अग्रिम अनुमान हैं। *2014-15 में अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा की उपज जुड़कर 1,070 किलो प्रति हेक्टेयर होती है।
स्रोत: एक नजर में कृषि सांख्यिकी, 2015, कृषि मंत्रालय; पीआरएस।
तालिका 14: राज्यों में सूक्ष्म सिंचाई का कवरेज (हेक्टेयर में)
|
राज्य/केंद्र शासित प्रदेश |
ड्रिप |
स्प्रिंकलर |
कुल |
सूक्ष्म सिंचाई के तहत बुवाई वाले क्षेत्र का % |
|
आंध्र प्रदेश |
8,34,865 |
3,28,441 |
11,63,306 |
10.5% |
|
अरुणाचल प्रदेश |
613 |
- |
613 |
0.3% |
|
असम |
310 |
129 |
439 |
0% |
|
बिहार |
4,610 |
97,440 |
1,02,050 |
1.9% |
|
छत्तीसगढ़ |
15,553 |
2,41,420 |
2,56,973 |
5.5% |
|
गोवा |
965 |
899 |
1,864 |
1.4% |
|
गुजरात |
4,11,208 |
4,18,165 |
8,29,373 |
8.1% |
|
हरियाणा |
22,682 |
5,50,458 |
5,73,140 |
16.3% |
|
हिमाचल प्रदेश |
291 |
684 |
975 |
0.2% |
|
झारखंड |
6,303 |
9,919 |
16,222 |
2.2% |
|
कर्नाटक |
4,29,903 |
4,17,005 |
8,46,908 |
60.2% |
|
केरल |
22,516 |
6,948 |
29,464 |
0.3% |
|
मध्य प्रदेश |
1,66,358 |
1,85,759 |
3,52,117 |
17.2% |
|
महाराष्ट्र |
8,96,343 |
3,74,783 |
12,71,126 |
8.3% |
|
मणिपुर |
47 |
30 |
77 |
0% |
|
मिजोरम |
1,727 |
425 |
2,152 |
0.7% |
|
नागालैंड |
200 |
5,005 |
5,205 |
1.8% |
|
ओड़िशा |
18,431 |
82,147 |
1,00,578 |
86.7% |
|
पंजाब |
30,805 |
12,161 |
42,966 |
11.3% |
|
राजस्थान |
1,70,098 |
15,14,451 |
16,84,549 |
38.4% |
|
सिक्किम |
5,544 |
2,769 |
8,313 |
0.2% |
|
तमिलनाडु |
2,90,009 |
30,436 |
3,20,445 |
1.8% |
|
तेलंगाना |
25,299 |
5,293 |
30,592 |
39.7% |
|
त्रिपुरा |
100 |
392 |
492 |
0% |
|
उत्तर प्रदेश |
15,519 |
21,164 |
36,683 |
14.3% |
|
उत्तराखंड |
696 |
316 |
1,012 |
0.1% |
|
पश्चिम बंगाल |
604 |
50,576 |
51,180 |
0.3% |
|
अन्य |
15,500 |
31,000 |
46,500 |
0.9% |
|
भारत |
33,87,099 |
43,88,215 |
77,75,314 |
5.6% |
स्रोत: तालिका 15.2 (क) एक नजर में कृषि सांख्यिकी, 2015, कृषि मंत्रालय; पीआरएस।
तालिका 15: राज्यों में भूजल विकास और सिंचाई का कवरेज
|
राज्य |
भूजल विकास (%) |
सिंचाई क्षेत्र का % |
|
आंध्र प्रदेश |
45% |
38.0% |
|
अरुणाचल प्रदेश |
0% |
13.0% |
|
असम |
14% |
5.4% |
|
बिहार |
44% |
47.8% |
|
छत्तीसगढ़ |
35% |
26.4% |
|
गोवा |
28% |
40.4% |
|
गुजरात |
137% |
41.2% |
|
हिमाचल प्रदेश |
71% |
11.4% |
|
हरियाणा |
67% |
90.2% |
|
झारखंड |
21% |
3.7% |
|
जम्मू और कश्मीर |
133% |
39.9% |
|
कर्नाटक |
32% |
26.9% |
|
केरल |
64% |
22.2% |
|
महाराष्ट्र |
57% |
16.7% |
|
मेघालय |
0% |
20.9% |
|
मणिपुर |
1% |
18.6% |
|
मध्य प्रदेश |
47% |
43.8% |
|
मिजोरम |
4% |
9.5% |
|
नागालैंड |
6% |
7.0% |
|
ओड़िशा |
28% |
26.2% |
|
पंजाब |
172% |
99.5% |
|
राजस्थान |
26% |
31.9% |
|
सिक्किम |
137% |
15.9% |
|
तमिलनाडु |
77% |
50.2% |
|
त्रिपुरा |
7% |
21.4% |
|
उत्तराखंड |
74% |
40.9% |
|
उत्तर प्रदेश |
57% |
76.2% |
|
पश्चिम बंगाल |
40% |
62.2% |
|
सभी राज्य |
62% |
47.2% |
स्रोत: केंद्रीय जल आयोग, कृषि गणना 2011; पीआरएस।
तालिका 16: अक्टूबर 2016 तक राज्यों में भूमि पट्टे की कानूनी स्थिति
|
राज्य/केंद्र शासित प्रदेश |
भूमि पट्टे संबंधी रोक |
नए भूमि पट्टा कानून को मंजूरी |
|
आंध्र प्रदेश |
आंशिक |
नहीं |
|
अरुणाचल प्रदेश |
प्रतिबंधित |
नहीं |
|
असम |
आंशिक |
नहीं |
|
बिहार |
प्रतिबंधित |
नहीं |
|
छत्तीसगढ़ |
प्रतिबंधित |
नहीं |
|
गोवा |
प्रतिबंधित |
नहीं |
|
गुजरात |
प्रतिबंधित |
नहीं |
|
हरियाणा |
आंशिक |
नहीं |
|
हिमाचल प्रदेश |
प्रतिबंधित |
नहीं |
|
जम्मू और कश्मीर |
प्रतिबंधित |
नहीं |
|
झारखंड |
प्रतिबंधित |
नहीं |
|
कर्नाटक |
प्रतिबंधित |
नहीं |
|
केरल |
प्रतिबंधित |
नहीं |
|
मध्य प्रदेश |
- |
हां |
|
महाराष्ट्र |
आंशिक |
नहीं |
|
मणिपुर |
प्रतिबंधित |
नहीं |
|
मेघालय |
प्रतिबंधित |
नहीं |
|
मिजोरम |
प्रतिबंधित |
नहीं |
|
नागालैंड |
प्रतिबंधित |
नहीं |
|
ओड़िशा |
प्रतिबंधित |
नहीं |
|
पंजाब |
आंशिक |
नहीं |
|
राजस्थान |
आंशिक |
नहीं |
|
सिक्किम |
प्रतिबंधित |
नहीं |
|
तमिलनाडु |
आंशिक |
नहीं |
|
तेलंगाना |
प्रतिबंधित |
नहीं |
|
त्रिपुरा |
आंशिक |
नहीं |
|
उत्तर प्रदेश |
आंशिक |
नहीं |
|
उत्तराखंड |
प्रतिबंधित |
नहीं |
|
पश्चिम बंगाल |
आंशिक |
नहीं |
|
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह |
प्रतिबंधित |
नहीं |
|
चंडीगढ़ |
प्रतिबंधित |
नहीं |
|
दादरा और नगर हवेली |
प्रतिबंधित |
नहीं |
|
दमन और दीव |
प्रतिबंधित |
नहीं |
|
दिल्ली |
प्रतिबंधित |
नहीं |
|
लक्षदीप |
प्रतिबंधित |
नहीं |
|
पुद्दूचेरी |
प्रतिबंधित |
नहीं |
स्रोत: भारतीय राज्यों में कृषि मार्केटिंग और किसान अनुकूल सुधार पर स्टडी रिपोर्ट, नीति आयोग; पीआरएस।
तालिका 17: 2005-2016 के दौरान मुख्य फसलों के लिए एमएसपी (रुपए/क्विंटल में)
|
फसल |
2005-06 |
2010-11 |
2016-17 |
2010-11 से 2016-17 में हुई वृद्धि का % |
2005-06 से 2016-17 में हुई वृद्धि का % |
|
धान सामान्य |
570 |
1,000 |
1,470 |
6.6% |
9.0% |
|
ज्वार हाइब्रिड |
525 |
880 |
1,625 |
10.8% |
10.8% |
|
मक्का |
540 |
880 |
1,365 |
7.6% |
8.8% |
|
रागी |
525 |
965 |
1,725 |
10.2% |
11.4% |
|
तुअर (अरहर) |
1,400 |
3,500 |
5,050 |
6.3% |
12.4% |
|
मूंग |
1,520 |
3,670 |
5,225 |
6.1% |
11.9% |
|
उड़द |
1,520 |
3,400 |
5,000 |
6.6% |
11.4% |
|
मूंगफली छिलका सहित |
1,520 |
2,300 |
4,220 |
10.6% |
9.7% |
|
तिल |
1,520 |
2,900 |
5,000 |
9.5% |
11.4% |
|
कपास मध्यम रेशा |
1,760 |
2,500 |
3,860 |
7.5% |
7.4% |
|
कपास लंबा रेशा |
1,980 |
3,000 |
4,160 |
5.6% |
7.0% |
|
गेहूं |
700 |
1,170 |
1,625 |
5.6% |
8.0% |
|
मसूर |
1,535 |
2,250 |
3,950 |
9.8% |
9.0% |
|
रैपीसीड/सरसों |
1,715 |
1,850 |
3,700 |
12.2% |
7.2% |
नोट: एमएसपी में कुछ फसलों के लिए घोषित बोनस शामिल है।
स्रोत: आर्थिक और सांख्यिकी निदेशालय, कृषि मंत्रालय; पीआरएस।
तालिका 18: अक्टूबर 2016 तक राज्यों में एपीएमसी सुधारों की स्थिति
|
राज्य/केंद्र शासित प्रदेश |
एपीएमसी से बाहर फल और सब्जियां |
कृषि उत्पादों पर टैक्स |
उत्पादकों द्वारा सीधी बिक्री |
ई-नैम |
नैम के तहत आने वाले बाजारों की संख्या |
|
आंध्र प्रदेश |
नहीं किया गया |
7.0% |
हां |
हां |
5 |
|
अरुणाचल प्रदेश |
नहीं किया गया |
2.0% |
हां |
नहीं |
0 |
|
असम |
किया गया |
1.0% |
हां |
नहीं |
0 |
|
बिहार |
नहीं किया गया |
0.0% |
नहीं |
नहीं |
0 |
|
छत्तीसगढ़ |
आंशिक रूप से |
2.0% |
हां |
हां |
12 |
|
गोवा |
नहीं किया गया |
5.0% |
हां |
नहीं |
0 |
|
गुजरात |
किया गया |
5.8% |
हां |
हां |
40 |
|
हरियाणा |
आंशिक रूप से |
10.5% |
हां |
हां |
36 |
|
हिमाचल प्रदेश |
आंशिक रूप से |
7.0% |
हां |
हां |
7 |
|
जम्मू और कश्मीर |
नहीं किया गया |
0.0% |
नहीं |
नहीं |
0 |
|
झारखंड |
नहीं किया गया |
5.3% |
हां |
हां |
8 |
|
कर्नाटक |
आंशिक रूप से |
7.5% |
हां |
नहीं |
0 |
|
केरल |
नहीं किया गया |
3.0% |
नहीं |
नहीं |
0 |
|
मध्य प्रदेश |
आंशिक रूप से |
2.0% |
हां |
हां |
20 |
|
महाराष्ट्र |
आंशिक रूप से |
3.0% |
हां |
हां |
0 |
|
मणिपुर |
नहीं किया गया |
0.0% |
नहीं |
नहीं |
0 |
|
मेघालय |
किया गया |
1.0% |
नहीं |
नहीं |
0 |
|
मिजोरम |
नहीं किया गया |
0.0% |
हां |
नहीं |
0 |
|
नागालैंड |
आंशिक रूप से |
0.0% |
हां |
नहीं |
0 |
|
ओड़िशा |
किया गया |
5.5% |
नहीं |
नहीं |
0 |
|
पंजाब |
नहीं किया गया |
13.5% |
हां |
नहीं |
0 |
|
राजस्थान |
आंशिक रूप से |
2.8% |
हां |
हां |
11 |
|
सिक्किम |
नहीं किया गया |
1.3% |
हां |
नहीं |
0 |
|
तमिलनाडु |
नहीं किया गया |
5.0% |
नहीं |
नहीं |
0 |
|
तेलंगाना |
नहीं किया गया |
0.0% |
हां |
हां |
44 |
|
त्रिपुरा |
नहीं किया गया |
2.0% |
हां |
नहीं |
0 |
|
उत्तर प्रदेश |
नहीं किया गया |
4.0% |
नहीं |
हां |
66 |
|
उत्तराखंड |
नहीं किया गया |
9.0% |
हां |
नहीं |
0 |
|
पश्चिम बंगाल |
आंशिक रूप से |
5.0% |
हां |
नहीं |
0 |
|
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह |
नहीं किया गया |
0.0% |
नहीं |
नहीं |
0 |
|
चंडीगढ़ |
नहीं किया गया |
10.5% |
हां |
नहीं |
0 |
|
दादरा और नगर हवेली |
नहीं किया गया |
0.0% |
नहीं |
नहीं |
0 |
|
दमन और दीव |
नहीं किया गया |
0.0% |
नहीं |
नहीं |
0 |
|
दिल्ली |
आंशिक |
7.0% |
नहीं |
नहीं |
0 |
|
लक्षदीप |
नहीं किया गया |
0.0% |
नहीं |
नहीं |
0 |
|
पुद्दूचेरी |
नहीं किया गया |
4.8% |
नहीं |
नहीं |
0 |
स्रोत: भारतीय राज्यों में कृषि मार्केटिंग और किसान अनुकूल सुधार पर स्टडी रिपोर्ट, नीति आयोग; पीआरएस।
[1] Table 10, Employment across various sectors, Report of the 12th Plan Working Group on Employment, Planning and Policy, December 2011, http://planningcommission.gov.in/aboutus/committee/wrkgrp12/wg_emp_planing.pdf.
[2] Press Note on First Revised Estimates of National Income, 2015-16, Ministry of Statistics and Programme Implementation, January 31, 2017, http://mospi.nic.in/sites/default/files/press_release/nad_PR_31jan17.pdf.
[3] Tables 1.3A and 1.3B, Statistical Appendix, Economic Survey 2015-16, http://unionbudget.nic.in/es2015-16/estat1.pdf.
[4] Fourth Advance Estimates of Production of Food grains for 2015-16, Directorate of Economics and Statistics, Ministry of Agriculture, August 17, 2015, http://eands.dacnet.nic.in/Advance_Estimate/4th_Adv2014-15Eng.pdf.
[5] Second Advance Estimates of Production of Food Grains for 2016-17, Directorate of Economics and Statistics, Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, February 15, 2017, http://eands.dacnet.nic.in/Advance_Estimate/2nd_Advance_Estimate_ENG.pdf.
[6] 29th Report: Impact of Chemical Fertilizers and Pesticides on Agriculture and allied sectors in the country, Standing Committee on Agriculture, August 11, 2016, http://164.100.47.134/lsscommittee/Agriculture/16_Agriculture_29.pdf.
[7] Table 4.4: Season-wise Area, Production and Yield of food grains, Agricultural Statistics at a Glance 2015, http://eands.dacnet.nic.in/PDF/Agricultural_Statistics_At_Glance-2015.pdf...
[8] Table 7.2, Agricultural Statistics at a Glance 2015, http://eands.dacnet.nic.in/PDF/Agricultural_Statistics_At_Glance-2015.pdf...
[9] Food and Agricultural Organisation of the United Nations, http://www.fao.org/faostat/en/#compare.
[10] “Food Security”, Policy Brief, Issue 2, June 2006, Food and Agriculture Organisation, United Nations, http://www.fao.org/forestry/13128-0e6f36f27e0091055bec28ebe830f46b3.pdf.
[11] “The State of Food Insecurity in the World, 2015”, Food and Agriculture Organization of the United Nations, http://www.fao.org/3/a-i4646e.pdf.
[12] “Food Management”, Chapter 5: Prices, Agriculture and Food Management, Economic Survey 2015-16, http://unionbudget.nic.in/es2015-16/echapvol2-05.pdf.
[13] National Food Security Act, 2013, Department of Food and Public Distribution, Ministry of Food and Public Distribution, http://dfpd.nic.in/writereaddata/Portal/Magazine/Document/1_43_1_NFS-Act-English.pdf.
[14] National Food Security Act, 2013, Food Grains Bulletin December 2015, Department of Food and Public Distribution, Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, http://dfpd.nic.in/writereaddata/images/EstdStatewiseNFSA.pdf.
[15] “Nutritional Intake in India, 2011-12”, NSS 68th Round (July 2011 to June 2012), National Sample Survey Office, Ministry of Statistics and Programme Implementation, October 2014, http://mospi.nic.in/sites/default/files/publication_reports/nss_report_560_19dec14.pdf.
[16] “Incentivising productivity of pulses through minimum support prices”, Ministry of Finance, September 16, 2016, http://finmin.nic.in/reports/Pulses_report_16th_sep_2016.pdf.
[17] Table 12.1, Agricultural Statistics at a Glance 2015, Ministry of Agriculture, http://eands.dacnet.nic.in/PDF/Agricultural_Statistics_At_Glance-2015.pdf.
[18] Chapter 5, Prices, Agriculture and Food Management, Volume 2, Economic Survey 2015-16, http://unionbudget.nic.in/es2015-16/echapvol2-05.pdf.
[19] Table 13.1: Agricultural Land by use in India, Agricultural Statistics at a Glance 2015, http://eands.dacnet.nic.in/PDF/Agricultural_Statistics_At_Glance-2015.pdf..
[20] Agriculture Census 2010-11, http://agcensus.nic.in/document/agcensus2010/completereport.pdf.
[21] Report of the Expert Committee on Land Leasing, NITI Aayog, March 31, 2016, http://www.niti.gov.in/writereaddata/files/document_publication/Final_Report_Expert_Group_on_Land_Leasing.pdf.
[22] Frequently Asked Questions, Bhoomi, Government of Karnataka, http://bhoomi.karnataka.gov.in/faq.htm.
[23] Part XV, Agrarian Reforms, Report of the National Commission on Agriculture, 1976, Ministry of Agriculture, http://krishikosh.egranth.ac.in/bitstream/1/2041446/1/CCS320.pdf.
[24] Study Report on Agricultural Marketing and Farmer Friendly Reforms Across Indian States and UTs, October 2016, NITI Aayog, http://www.niti.gov.in/writereaddata/files/document_publication/Index_Agri_reform_%20Oct2016.pdf.
[25] Report of the Committee on Medium-term Path on Financial Inclusion, Reserve Bank of India, December 2015, https://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/PublicationReport/Pdfs/FFIRA27F4530706A41A0BC394D01CB4892CC.PDF.
[26] Report of the Internal Working Group to Revisit the Existing Priority Sector Lending Guidelines, Reserve Bank of India, March 2, 2015, https://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/PublicationReport/Pdfs/PSGRE020315.pdf.
[27] Report of the Advisory Committee on Flow of Credit to Agriculture, Reserve Bank of India, May 2004, https://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/PublicationReport/Pdfs/53525.pdf.
[28] 12th Plan Working Group Report on Natural Resource Management and Rainfed Farming, November 15, 2011.
[29] 34th Report: State of rural/agricultural banking and crop insurance, Standing Committee on Finance, August 10, 2016, http://164.100.47.134/lsscommittee/Finance/16_Finance_34.pdf.
[30] “Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana (PMFBY), Ministry of Agriculture, http://agricoop.nic.in/imagedefault/whatsnew/sch_eng.pdf; “Cabinet approves New Crop Insurance Scheme – Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana”, Press Information Bureau, Ministry of Agriculture, January 13, 2016.
[31] Expenditure Budget Volume 2, Department of Agriculture and Co-operation, Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Union Budget 2016-17, http://unionbudget.nic.in/ub2016-17/eb/sbe1.pdf.
[32] Expenditure Profile, Union Budget 2017-18, http://unionbudget.nic.in/vol1.asp.
[33] Lok Sabha Starred Question no. 196, Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Answered on November 29, 2016, http://164.100.47.194/Loksabha/Questions/QResult15.aspx?qref=42786&lsno=16.
[34] Union Budget 2017-18 Budget Speech, http://unionbudget.nic.in/ub2017-18/bs/bs.pdf.
[35] “Achievements of Ministry of Agriculture and Farmers Welfare”, Press Information Bureau, Ministry of Agriculture, January 2, 2017.
[36] Pocket Book of Agricultural Statistics, 2015, Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, http://eands.dacnet.nic.in/PDF/Pocket-Book2015.pdf.
[37] “Raising Agricultural Productivity and Making Farming Remunerative for Farmers”, NITI Aayog, December 16, 2015, http://www.niti.gov.in/writereaddata/files/document_publication/RAP3.pdf.
[38] Water and Related Statistics 2015, Central Water Commission, April 2015, http://www.cwc.gov.in/main/downloads/Water%20&%20Related%20Statistics%202015.pdf.
[39] Recommendations for Price Policy, Price Policy for Kharif Crops 2015-16, Commission for Agricultural Costs and Prices, Ministry of Agriculture, March 2015, http://cacp.dacnet.nic.in/ViewReports.aspx?Input=2&PageId=40&KeyId=532.
[40] Draft Model Bill for the Conservation, Protection and Regulation of Groundwater, http://www.planningcommission.nic.in/aboutus/committee/wrkgrp12/wr/wg_model_bill.pdf; ‘
Draft National Water Framework Bill, 2013, Ministry of Water Resources, http://www.indiaenvironmentportal.org.in/files/file/Draft%20national%20framework%20bill,%202013.pdf.
[41] National Water Policy, 2012, http://wrmin.nic.in/writereaddata/NationalWaterPolicy/NWP2012Eng6495132651.pdf.
[42] Model Bill for the Conservation, Protection, Regulation and Management of Ground Water Bill, 2016, Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation, http://wrmin.nic.in/writereaddata/Model_Bill_Groundwater_May_2016.pdf.
[43] “Chapter 4: Agriculture: More from less”, Economic Survey 2015-16, http://unionbudget.nic.in/es2015-16/echapvol1-04.pdf.
[44] Natural Resource Management, State of Indian Agriculture 2015-16, Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, May 2016, http://agricoop.nic.in/imagedefault/state_agri_1516.pdf.
[45] “Compendium on Soil Health”, Ministry of Agriculture, January 2012, http://agricoop.nic.in/Admin_Agricoop/Uploaded_File/Comsoilhealth28612.pdf. I
[46] Soil and its Survey, State of Indian Agriculture 2015-16, Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, May 2016, http://eands.dacnet.nic.in/PDF/State_of_Indian_Agriculture,2015-16.pdf.
[47] Progress Report for states, Soil Health Card scheme website, Department of Agriculture, Co-operation and Farmers Welfare, February 15, 2017, http://soilhealth.dac.gov.in/PublicReports/StateWiseSampleEnteredTestedSHCPrintedDateFromTo. .
[48] Lok Sabha Unstarred Question no. 755, Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Answered on February 7, 2017.
[49] Chapter 9, Volume 1, Reforming the Fertiliser Sector, Economic Survey 2015-16, http://unionbudget.nic.in/es2015-16/echapvol1-09.pdf
[50] Report No. 16 of 2015, Performance Audit on Nutrient Based Subsidy Policy, http://cag.gov.in/content/report-no-16-2015-performace-audit-nutrient-based-subsidy-policy-decontrolled-phosphatic.
[51] Report of the High Level Committee on Reorienting the role and restructuring the Food Corporation of India, January 2015, http://www.fci.gov.in/app/webroot/upload/News/Report%20of%20the%20High%20Level%20Committee%20on%20Reorienting%20the%20Role%20and%20Restructuring%20of%20FCI_English_1.pdf.
[52] Budget Speech, Union Budget 2016-17, http://unionbudget.nic.in/ub2016-17/bs/bs.pdf.
[53] “Department of Fertilizers to conduct pilot in 16 districts to capture details as a precursor to DBT in fertilizer sector”, Press Information Bureau, Ministry of Chemicals and Fertilizers, July 29, 2016.
[54] Farm Inputs and Management, State of Indian Agriculture 2015-16, Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, May 2016, http://agricoop.nic.in/imagedefault/state_agri_1516.pdf.
[55] “Indian seed sector”, Seednet India Portal, Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, http://seednet.gov.in/Material/IndianSeedSector.htm.
[56] Productivity through seed development, Chapter 5, Agriculture and Food Management, Volume 2, Economic Survey 2015-16, http://unionbudget.nic.in/es2015-16/echapvol2-05.pdf.
[57] State of Indian Agriculture 2015-16, Ministry of Agriculture, http://eands.dacnet.nic.in/PDF/State_of_Indian_Agriculture,2015-16.pdf.
[58] Table 4.21(a), Agricultural Statistics at a Glance 2015, http://eands.dacnet.nic.in/PDF/Agricultural_Statistics_At_Glance-2015.pdf...
[59] GEAC clearances, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, http://envfor.nic.in/major-initiatives/geac-clearances.
[60] “GEAC invites comments for the proposal on authorisation of environmental release of Genetically Engineered Mustard”, Press Information Bureau, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, September 6, 2016.
[61] “Assessment of Food and Environmental Safety”, Environmental release of Genetically Engineered Mustard hybrid DMH-11, Ministry of Environment, Forests and Climate Change, September 2016, http://www.moef.gov.in/sites/default/files/Safety%20assessment%20report%20on%20GE%20Mustard_0.pdf.
[62] Mechanization and Technology, Chapter 8, Agriculture and Food Management, Economic Survey 2013-14, http://unionbudget.nic.in/budget2014-2015/es2013-14/echap-08.pdf.
[63] Mechanization, Chapter 5, Prices, Agriculture and Food Management, Volume 2, Economic Survey 2015-16, http://unionbudget.nic.in/es2015-16/echapvol2-05.pdf.
[64] “Audit on the Preparedness for the Implementation of National Food Security Act, 2013”, Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, Comptroller and Auditor General of India, April 2016, http://www.cag.gov.in/sites/default/files/audit_report_files/Union_Civil_National_Food_Security_Report_54_of_2015.pdf.
[65] Storage, Department of Food and Public Distribution, http://dfpd.nic.in/storage-intro.htm.
[66] Storage of Food Grains, State of Indian Agriculture 2015-16, Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, May 2016, http://agricoop.nic.in/imagedefault/state_agri_1516.pdf.
[67] Annual Report 2014-15, Warehousing Development and Regulatory Authority, http://wdra.nic.in/Annual-report2014-15%20English.pdf.
[68] Cold storage, Tamil Nadu Agricultural University Agritech Portal, http://agritech.tnau.ac.in/agricultural_marketing/agrimark_cold%20storage.html.
[69] “Challenges to cold chain development”, National Centre for Cold-Chain Development, 2012, http://www.nccd.gov.in/PDF/ChallengeColdChain-Development.pdf.
[70] Report on Evaluation of the Impact of the Scheme for Mega Food Park of the Ministry of Food Processing, Indian Council for Research for International Economic Relations, July 2015, http://mofpi.nic.in/sites/default/files/ICRIERreportonimpactofMFPS%28Final%29_0.pdf.
[71] “Food Processing Units and Mega Food Parks”, Press Information Bureau, Ministry of Food Processing Industries, July 29, 2016.
[72] Department of Food and Public Distribution, Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution.
[73] “Pricing, Costs, Returns and Productivity in Indian Crop Sector during 2000s”, Commission for Agriculture Costs and Prices, Ministry of Agriculture, June 2013, http://cacp.dacnet.nic.in/ViewQuestionare.aspx?Input=2&DocId=1&PageId=42&KeyId=480.
[74] Evaluation Report on Efficacy of Minimum Support Prices (MSPs), NITI Aayog, January 2016, http://www.niti.gov.in/writereaddata/files/document_publication/MSP-report.pdf.
[75] The Essential Commodities Act, 1955, http://seednet.gov.in/PDFFILES/Essential_Commodity_Act_1955(No_10_of_1955).pdf.
[76] Agricultural Marketing, Department of Agriculture, Co-operation and Farmers Welfare, Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, http://www.agricoop.nic.in/divisiontype/agricultural-marketing.
[77] Salient Features of the Model Act on Agricultural Marketing, Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, http://agmarknet.nic.in/amrscheme/modelact.htm.
[78] Agricultural Prices, Marketing and International Trade, State of Indian Agriculture 2015-16, Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, May 2016, http://agricoop.nic.in/imagedefault/state_agri_1516.pdf.
[79] Chapter 8, “A National Market for Agricultural Commodities – Some Issues and the Way Forward”, Volume 1, Economic Survey 2014-15, http://www.indiabudget.nic.in/es2014-15/echapvol1-08.pdf.
[80] “The Prime Minister launched National Agricultural Market”, Press Information Bureau, April 14, 2016.
अस्वीकरणः प्रस्तुत रिपोर्ट आपके समक्ष सूचना प्रदान करने के लिए प्रस्तुत की गई है। पीआरएस लेजिसलेटिव रिसर्च (पीआरएस) की स्वीकृति के साथ इस रिपोर्ट का पूर्ण रूपेण या आंशिक रूप से गैर व्यावसायिक उद्देश्य के लिए पुनःप्रयोग या पुनर्वितरण किया जा सकता है। रिपोर्ट में प्रस्तुत विचार के लिए अंततः लेखक या लेखिका उत्तरदायी हैं। यद्यपि पीआरएस विश्वसनीय और व्यापक सूचना का प्रयोग करने का हर संभव प्रयास करता है किंतु पीआरएस दावा नहीं करता कि प्रस्तुत रिपोर्ट की सामग्री सही या पूर्ण है। पीआरएस एक स्वतंत्र, अलाभकारी समूह है। रिपोर्ट को इसे प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के उद्देश्यों अथवा विचारों से निरपेक्ष होकर तैयार किया गया है। यह सारांश मूल रूप से अंग्रेजी में तैयार किया गया था। हिंदी रूपांतरण में किसी भी प्रकार की अस्पष्टता की स्थिति में अंग्रेजी के मूल सारांश से इसकी पुष्टि की जा सकती है।