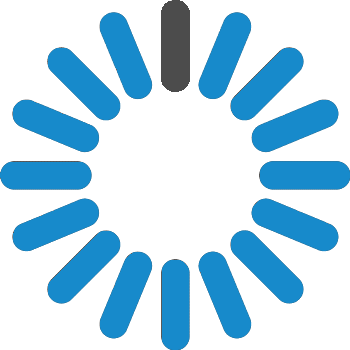स्टैंडिंग कमिटी की रिपोर्ट का सारांश
- कार्मिक, जन शिकायत, विधि एवं न्याय संबंधी स्टैंडिंग कमिटी (चेयर: भूपेंद्र यादव) ने 11 सितंबर, 2020 को वर्चुअल न्यायालयों की कार्य पद्धति पर अपनी रिपोर्ट सौंपी। कमिटी ने इस बात पर जोर दिया कि देश के इकोसिस्टम में वर्चुअल न्यायालयों को एकीकृत करने की जरूरत है। मुख्य सुझावों में निम्नलिखित शामिल हैं:
- डिजिटल डिवाइड: कमिटी ने कहा कि बड़े पैमाने पर वकीलों और वादियों को बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर और हाई स्पीड इंटरनेट उपलब्ध नहीं है जोकि वर्चुअल सुनवाई के लिए जरूरी हैं। कमिटी ने सुझाव दिया कि इस समस्या को हल करने के लिए निजी एजेंसियों को शामिल करने की संभावनाओं को तलाशा जाना चाहिए ताकि वे उन लोगों तक वीडियो कांफ्रेंसिंग के उपकरण लेकर जाएं जो टेक सैवी नहीं हैं। इससे वे लोग अदालतों से कनेक्ट कर पाएंगे। कमिटी ने यह सुझाव भी दिया कि न्यायपालिका को सुदूर क्षेत्रों में मोबाइल वीडियो कांफ्रेंसिंग सुविधाओं को शुरू करने पर विचार करना चाहिए।
- कनेक्टिविटी डिवाइड: कमिटी ने सुझाव दिया कि सरकार को राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन को समय पर लागू करने के लिए कोशिशें तेज करनी चाहिए। इस मिशन का उद्देश्य डिजिटल कम्यूनिकेशंस इंफ्रास्ट्रक्टर की वृद्धि को तेज करना, डिजिटल डिवाइड को दूर करना और सभी को सार्वभौमिक एवं सस्ती ब्रॉडबैंड सुविधा प्रदान करना है।
- स्किल डिवाइड: कमिटी ने कहा कि देश के सभी अदालती परिसरों में प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाने चाहिए ताकि वकीलों को डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर काम करने के लिए जरूरी दक्षताएं हासिल हों। कमिटी ने यह सुझाव भी दिया कि भारतीय बार काउंसिल को कॉलेजों के लॉ कोर्सेज़ में कंप्यूटर कोर्स को विषय के तौर पर शुरू करना चाहिए ताकि स्टूडेंट्स ऑनलाइन प्रणाली को अपना सकें।
- अधीनस्थ अदालतें: कमिटी ने कहा कि निचली अदालतों में बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं है और उन्हें वर्चुअल अदालतों को अपनाने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। चूंकि वर्चुअल अदालतों में शुरुआत में अधिक निवेश की जरूरत होती है, इसलिए कमिटी ने सुझाव दिया कि वित्त पोषण के नए तरीकों की संभावनाओं की तलाश की जानी चाहिए जैसे सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल। उसने यह सुझाव भी दिया कि भारतीय बार काउंसिल को संबंधित राज्य बार काउंसिल्स को सलाह देनी चाहिए। उनसे कहना चाहिए कि वे वर्चुअल अदालतों के संबंध में वकीलों के लिए क्रैश कोर्स की व्यवस्था करें। वे समाज के कमजोर तबकों के वकीलों की समस्याओं को दूर करने के बारे में सोचें। इससे उन्हें इस अवधि के दौरान वर्चुअल सुनवाइयों के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर हासिल करने में मदद मिलेगी।
- ई-कोर्ट प्रॉजेक्ट: ई-कोर्ट प्रॉजेक्ट का उद्देश्य भारत के सभी न्यायालयों में आईसीटी (इनफॉरमेशन एंड कम्यूनिकेशन टेक्नोलॉजी) के एनेबलमेंट को सुनिश्चित करना है। कमिटी ने कहा कि प्रॉजेक्ट की रफ्तार बहुत धीमी है। उसने सुझाव दिया कि न्याय विभाग (विधि एवं न्याय मंत्रालय के अंतर्गत) को यह सुनिश्चित करने के लिए जरूरी कदम उठाने चाहिए कि प्रॉजेक्ट के अंतर्गत लक्ष्यों को निश्चित समय सीमा में हासिल किया जाए।
- स्वदेशी सॉफ्टवेयर: कमिटी ने कहा कि थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर के सुरक्षात्मक खतरे हो सकते हैं। उसने सुझाव दिया कि इलेक्ट्रॉनिक एवं इनफॉरमेशन टेक्नोलॉजी मंत्रालय को वर्चुअल अदालती सुनवाइयों के लिए स्वदेशी सॉफ्टवेयर विकसित करवाना चाहिए। कमिटी ने यह सुझाव भी दिया कि निजी कंपनियों को ऐसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम्स को विकसित करने में संलग्न किया जाना चाहिए जो बल्क डॉक्यूमेंटेशन कर सकें और ग्राफिक्स का उन्नत तरीके से इस्तेमाल कर सकें।
- विजुअलाइजेशन: अदालती कार्रवाइयों के विजुअलाइजेशन में सुधार के लिए कमिटी ने कोर्ट रूम डिजाइन पर अध्ययन करने का सुझाव दिया। साथ ही कहा कि भारतीय सेटिंग्स में वर्चुअल अदालती सुनवाइयों को आसान बनाने के लिए सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को कस्टमाइज किया जाए।
- ओपन कोर्ट्स: कमिटी ने सर्वोच्च न्यायालय के पिछले सुझाव पर सहमति जताई कि कार्रवाइयों की लाइव स्ट्रीमिंग होनी चाहिए, खासकर संवैधानिक और राष्ट्रीय महत्व के मामलों की। इससे पारदर्शिता और खुलापन आएगा। कमिटी ने यह सुझाव भी दिया कि न्यायपालिका को कुछ निश्चित श्रेणी के मामलों की वर्चुअल सुनवाइयों को ब्रॉडकास्ट करने पर विचार करना चाहिए जोकि ओपन जस्टिस के सिद्धांतों का आगे बढ़ाएगा।
- वर्चुअल न्यायालयों को जारी रखना: कमिटी ने सुझाव दिया कि कुछ निर्दिष्ट प्रकार की अपीलों और अंतिम सुनवाइयों (जहां शारीरिक उपस्थिति जरूरी नहीं) में सभी पक्षों की सहमति से प्रायोगिक आधार पर वर्चुअल सुनवाइयों की मौजूदा प्रणाली को जारी रखा जाए। कमिटी ने सुझाव दिया कि नेशनल कंपनी कानून अपीलीय ट्रिब्यूनल जैसे अपीलीय ट्रिब्यूनल्स में भी वर्चुअल न्यायालय के प्रारूप को अपनाया जाए क्योंकि वहां भी व्यक्तिगत हाजिरी की जरूरत नहीं है। उसने सुझाव दिया कि वर्चुअल न्यायालयों को एनेबल करने और वैध बनाने के लिए उपयुक्त संशोधन किए जाएं।
- आगे का रास्ता: कमिटी ने सुझाव दिया कि बार एसोसिएशंस और बार काउंसिल्स के सदस्यों की सलाह से पायलट आधार पर पूर्ण रूप से वर्चुअल न्यायालय प्रणाली को लागू किया जाए। उसने कहा कि न्याय विभाग ने ट्रैफिक चालान और चेक डिसऑनर जैसे मामलों को वर्चुअल न्यायालयों में स्थानांतरित करने का सुझाव दिया था। कमिटी ने यह सुझाव भी दिया कि जिन मामलों में व्यक्तिगत मौजूदगी की जरूरत नहीं है, उन सभी को वर्चुअल न्यायालयों में स्थानांतरित कर दिया जाना चाहिए। जिन मामलों में कानून, तथ्यों की व्याख्या करनी हो और बड़ी संख्या में चश्मदीदों की जांच करनी हो, उनमें मैनुअल प्रोसेस (जैसे शिकायत दर्ज करना और समन जारी करना) के डिजिटलीकरण के लिए हाइब्रिड मॉडल अपनाया जा सकता है और सुनवाई फिजिकल कोर्टरूम में की जा सकती है। इसके अतिरिक्त मध्यस्थता और सुलह संबंधी सुनवाइयों और समरी ट्रायल भी वर्चुअल न्यायालय में किए जा सकते हैं।
अस्वीकरणः प्रस्तुत रिपोर्ट आपके समक्ष सूचना प्रदान करने के लिए प्रस्तुत की गई है। पीआरएस लेजिसलेटिव रिसर्च (पीआरएस) के नाम उल्लेख के साथ इस रिपोर्ट का पूर्ण रूपेण या आंशिक रूप से गैर व्यावसायिक उद्देश्य के लिए पुनःप्रयोग या पुनर्वितरण किया जा सकता है। रिपोर्ट में प्रस्तुत विचार के लिए अंततः लेखक या लेखिका उत्तरदायी हैं। यद्यपि पीआरएस विश्वसनीय और व्यापक सूचना का प्रयोग करने का हर संभव प्रयास करता है किंतु पीआरएस दावा नहीं करता कि प्रस्तुत रिपोर्ट की सामग्री सही या पूर्ण है। पीआरएस एक स्वतंत्र, अलाभकारी समूह है। रिपोर्ट को इसे प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के उद्देश्यों अथवा विचारों से निरपेक्ष होकर तैयार किया गया है। यह सारांश मूल रूप से अंग्रेजी में तैयार किया गया था। हिंदी रूपांतरण में किसी भी प्रकार की अस्पष्टता की स्थिति में अंग्रेजी के मूल सारांश से इसकी पुष्टि की जा सकती है।