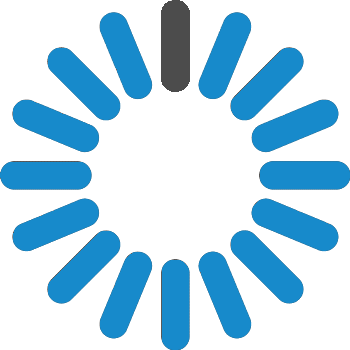लॉ कमीशन की रिपोर्ट का सारांश
- भारतीय लॉ कमीशन (चेयर: जस्टिस बी.एस.चौहान) ने न्यायालय अवमानना (कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स) एक्ट, 1971 पर अपनी रिपोर्ट सौंपी। अवमानना या कंटेम्प्ट न्यायालय की प्रतिष्ठा या अथॉरिटी के प्रति असम्मान प्रकट करने का अपराध है। एक्ट अवमानना या कंटेम्प्ट को सिविल और क्रिमिनल, दो हिस्सों में विभाजित करता है। सिविल कंटेम्प्ट का अर्थ यह है कि न्यायालय के किसी आदेश का जानबूझकर पालन न किया जाए। क्रिमिनल कंटेम्प्ट में ऐसे काम या पब्लिकेशंस शामिल हैं जो : (i) न्यायालय को ‘स्कैंडेलाइज’ करते हैं, या (ii) किसी न्यायिक प्रक्रिया को नकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं, या (iii) किसी भी प्रकार से न्याय की स्थापना में दखल देते हैं। ‘स्कैंडेलाइजिंग द कोर्ट’ का व्यापक अर्थ ऐसे बयान या पब्लिकेशंस हैं जो न्याय व्यवस्था में लोगों का भरोसा तोड़ते हैं।
- रिपोर्ट में इस बात की पड़ताल की गई कि क्या एक्ट में कंटेम्प्ट की परिभाषा को केवल सिविल कंटेम्प्ट तक सीमित रखा जाए यानी न्यायालय के फैसलों को जानबूझकर न मानना। कमीशन ने कहा कि एक्ट में संशोधन की कोई जरूरत नहीं है और इसके निम्नलिखित कारण हैं:
- कंटेम्प्ट के अत्यधिक मामले : कमीशन ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय और अनेक उच्च न्यायालयों में सिविल (96,993) और क्रिमिनल (583) कंटेम्प्ट के बहुत से मामले लंबित पड़े हैं। उसने कहा कि इतनी बड़ी संख्या में ऐसे मामलों की मौजूदगी से साबित होता है कि कानून की प्रासंगिकता बनी हुई है। कमीशन ने कहा कि कंटेम्प्ट की परिभाषा में संशोधन करने से कानून का असर और न्यायालयों, उनकी अथॉरिटी एवं कामकाज के प्रति लोगों में सम्मान कम होगा।
- अंतरराष्ट्रीय तुलना : ‘स्कैंडेलाइजिंग द कोर्ट’ के अपराध के संबंध में कमीशन ने युनाइटेड किंगडम का उदाहरण दिया। उसने कहा कि युनाइडेट किंगडम ने कंटेम्प्ट संबंधी अपने कानूनों से इस अपराध को हटा दिया है। हालांकि कमीशन ने यह भी कहा कि भारत और युनाइटेड किंगडम में दो अलग-अलग तरह की स्थितियां हैं जिससे प्रामाणित होता है कि इसे भारत में अपराध ही माना जाना चाहिए। पहला तो यह कि भारत में क्रिमिनल कंटेम्प्ट के मामलों की बहुत बड़ी संख्या है। जबकि यूके में स्कैंडेलाइजिंग द कोर्ट का आखिरी मामला 1931 में हुआ था। दूसरा, स्कैंडेलाइजिंग द कोर्ट यूके के दूसरे कानूनों में दंडनीय अपराध है। कमीशन ने कहा कि भारतीय कानून से इस अपराध को हटाने से लेजिसलेटिव गैप आ जाएगा, यानी कंटेम्प्ट के लिए कोई कानून नहीं बचेगा।
- कंटेम्प्ट से जुड़ी शक्ति का स्रोत क्या है: कमीशन ने कहा कि सुपीरियर कोर्ट्स (सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय) को कंटेम्प्ट से जुड़ी शक्तियां संविधान से मिली हुई हैं। एक्ट सिर्फ कंटेम्प्ट की जांच और सजा के संबंध में न्यायिक प्रक्रिया को रेखांकित करता है। इसलिए एक्ट से अपराध को हटाने से कंटेम्प्ट के मामलों में किसी को सजा देने की सुपीरियर कोर्ट्स की निहित संवैधानिक शक्तियों पर कोई असर नहीं होगा। ये शक्तियां 1971 के एक्ट से स्वतंत्र हैं, और बरकरार रहेंगी।
- सहायक न्यायालयों पर असर : संविधान सुपीरियर कोर्ट्स को उनका कंटेम्प्ट करने पर सजा देने की अनुमति देता है। इसके अतिरिक्त एक्ट उच्च न्यायालयों को इस बात की अनुमति देता है कि वे सहायक न्यायालयों का कंटेम्प्ट करने पर किसी को सजा दे सकते हैं। कमीशन का कहा है कि अगर कंटेम्प्ट की परिभाषा को सीमित किया जाएगा, तो सहायक न्यायालय प्रभावित होंगे, चूंकि उनके पास अपने कंटेम्प्ट के मामलों से निपटने का कोई उपाय नहीं होगा।
- अस्पष्टता : कमीशन ने कहा कि कंटेम्प्ट की परिभाषा में संशोधन करने से अस्पष्टता आएगी। इसका कारण यह होगा कि सुपीरियर कोर्ट्स संविधान के अंतर्गत कंटेम्प्ट संबंधी शक्तियों का इस्तेमाल करते रहेंगे। अगर एक्ट में क्रिमिनल कंटेम्प्ट की कोई परिभाषा नहीं रहेगी, तो सुपीरियर कोर्ट्स कंटेम्प्ट की अनेक परिभाषाएं और स्पष्टकीकरण दे सकते हैं। कमीशन ने सुझाव दिया कि स्पष्टता सुनिश्चित करने के लिए परिभाषा को बरकरार रखा जाए।
- पर्याप्त सेफगार्ड्स : कमीशन ने कहा कि एक्ट में दुरुपयोग रोकने के लिए अनेक सेफगार्ड्स दिए गए हैं। उदाहरण के लिए एक्ट के कई प्रावधानों में ऐसे मामले पेश किए गए हैं जो कंटेम्प्ट न माने जाएं और जिनमें कंटेम्प्ट सजा देने लायक नहीं होंगे। ये प्रावधान कहते हैं कि अदालतों में कंटेम्प्ट के सभी मामलों में मुकदमा नहीं चलाया जाएगा। इसके अतिरिक्त कमीशन ने कहा कि कई चुनौतियों के बावजूद एक्ट बना हुआ है, इसलिए उसमें संशोधन करने का कोई कारण नहीं है।
अस्वीकरणः प्रस्तुत रिपोर्ट आपके समक्ष सूचना प्रदान करने के लिए प्रस्तुत की गई है। पीआरएस लेजिसलेटिव रिसर्च (पीआरएस) की स्वीकृति के साथ इस रिपोर्ट का पूर्ण रूपेण या आंशिक रूप से गैर व्यावसायिक उद्देश्य के लिए पुनःप्रयोग या पुनर्वितरण किया जा सकता है। रिपोर्ट में प्रस्तुत विचार के लिए अंततः लेखक या लेखिका उत्तरदायी हैं। यद्यपि पीआरएस विश्वसनीय और व्यापक सूचना का प्रयोग करने का हर संभव प्रयास करता है किंतु पीआरएस दावा नहीं करता कि प्रस्तुत रिपोर्ट की सामग्री सही या पूर्ण है। पीआरएस एक स्वतंत्र, अलाभकारी समूह है। रिपोर्ट को इसे प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के उद्देश्यों अथवा विचारों से निरपेक्ष होकर तैयार किया गया है। यह सारांश मूल रूप से अंग्रेजी में तैयार किया गया था। हिंदी रूपांतरण में किसी भी प्रकार की अस्पष्टता की स्थिति में अंग्रेजी के मूल सारांश से इसकी पुष्टि की जा सकती है।