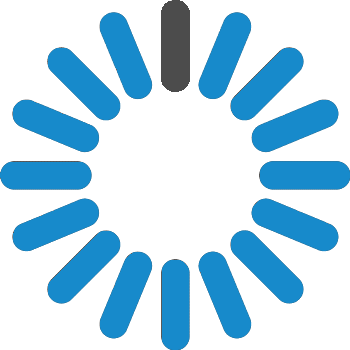रिपोर्ट का सारांश
-
वित्त मंत्री सुश्री निर्मला सीतारमण ने 31 जनवरी, 2025 को संसद में आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 पेश किया। सर्वेक्षण के मुख्य अंश इस प्रकार हैं:
अर्थव्यवस्था की स्थिति
-
सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी): आर्थिक सर्वेक्षण में 2025-26 में वास्तविक जीडीपी वृद्धि 6.3% से 6.8% के बीच रहने का अनुमान लगाया गया है। 2024-25 में भारत की वास्तविक जीडीपी 6.4% बढ़ने का अनुमान है। 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनने के लिए भारत को कम से कम एक दशक तक हर वर्ष लगभग 8% की निरंतर आर्थिक वृद्धि की आवश्यकता होगी। सतत निवेश, उपभोक्ता विश्वास में सुधार और कॉरपोरेट वेतन में बढ़ोतरी विकास को समर्थन देने के लिए महत्वपूर्ण होगी। ग्रामीण मांग और खाद्य मुद्रास्फीति में अनुमानित कमी से निकट अवधि में विकास को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। विकास के जोखिमों में कमोडिटीज़ की कीमतों में संभावित उतार-चढ़ाव और व्यापार एवं भूराजनैतिक अनिश्चतताओं का बढ़ना शामिल है। मध्यम अवधि की विकास क्षमता को सुदृढ़ करने के लिए भारत को संरचनात्मक सुधारों और रेगुलेशंस के जरिए अपनी वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार करने की आवश्यकता होगी।
-
मुद्रास्फीति: खुदरा मुद्रास्फीति 2023-24 में 5.4% से घटकर 2024-25 (अप्रैल-दिसंबर) में 4.9% हो गई। यह इनपुट की कीमतों में कमी के कारण है। भारत की खाद्य मुद्रास्फीति स्थिर बनी हुई है जो स्थिर या घटती खाद्य मुद्रास्फीति के वैश्विक रुझानों के अनुरूप नहीं है। खाद्य मुद्रास्फीति 2023-24 में 7.5% से बढ़कर 2024-25 (अप्रैल-दिसंबर) में 8.4% हो गई, जो मुख्य रूप से सब्जियों और दालों जैसी वस्तुओं के कारण थी। इसका कारण आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान और कुछ खाद्य पदार्थों की कम पैदावार को माना जा सकता है। खाद्यान्नों की तुलना में सब्जियां असमान मौसम के प्रति अधिक संवेदनशील होती हैं। दीर्घकालिक मूल्य स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए कुछ उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं: (i) जलवायु-अनुकूल फसल किस्मों को विकसित करना, (ii) किसानों को सर्वोत्तम कार्य पद्धतियों और उच्च उपज एवं रोग प्रतिरोधी बीजों के उपयोग का प्रशिक्षण देना, और (iii) व्यापक डेटा कलेक्शन और मूल्य एवं स्टॉक पर नज़र रखने के लिए विश्लेषण। सर्वेक्षण में कहा गया है कि आयातित वस्तुओं की गिरती कीमतें भारत की घरेलू मुद्रास्फीति के लिए अनुकूल हैं।
-
चालू खाता संतुलन: 2024-25 की दूसरी तिमाही में भारत का चालू खाता घाटा (सीएडी) जीडीपी का 1.2% था, जबकि 2023-24 की इसी तिमाही में जीडीपी का 1.3% था। सीएडी में हालिया वृद्धि को वस्तु व्यापार घाटे में वृद्धि के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। यह घाटा 2023-24 की इसी तिमाही में 65 बिलियन USD से बढ़कर 2024-25 की दूसरी तिमाही में 75 बिलियन USD हो गया। शुद्ध सेवा प्राप्तियों और निजी हस्तांतरण में वृद्धि से इसे मदद मिली। सर्वेक्षण में कहा गया है कि ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया जैसे अन्य देशों की तुलना में भारत का सीएडी अपेक्षाकृत नियंत्रित रहा है। प्रतिस्पर्धी बने रहने और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में भागीदारी में सुधार करने के लिए भारत को व्यापार लागत कम करना और निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार करना जारी रखना चाहिए।
-
सार्वजनिक वित्त: केंद्र सरकार के राजकोषीय अनुशासन के संकेतकों में उत्तरोत्तर सुधार हुआ है। केंद्र सरकार के कुल व्यय में पूंजीगत व्यय की हिस्सेदारी में 2020-21 से सुधार हुआ है और 2023-24 में यह 21% था। सर्वेक्षण में कहा गया है कि पिछले चार वर्षों में राजकोषीय प्रबंधन ने समग्र बचत-निवेश अंतर को बढ़ने से रोका। इससे घरेलू बचत में नरमी के बावजूद सीएडी का सुविधाजनक वित्तपोषण सुनिश्चित हुआ है।
कृषि एवं संबंधित गतिविधियां
-
कृषि क्षेत्र ने 2016-17 और 2022-23 के बीच 5% की वार्षिक औसत वृद्धि दर दर्ज की है। 2024-25 की दूसरी तिमाही में क्षेत्र 3.5% की दर से बढ़ा। 2024-25 की दूसरी तिमाही में इस क्षेत्र की वृद्धि दर 3.5% रही। इस क्षेत्र में सतत विकास को लाभकारी कीमतों, संस्थागत ऋण तक बेहतर पहुंच, उत्पादकता में वृद्धि और फसल विविधीकरण द्वारा मदद मिली है। पिछले एक दशक में कृषि आय में सालाना 5.2% की वृद्धि, जबकि गैर-कृषि आय में 6.2% की वृद्धि हुई है।
-
भारत में फसल की पैदावार अन्य देशों की तुलना में काफी कम है। यह उत्पादकता में सुधार की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है। फसल उत्पादकता खेती और फसल कटाई के बाद के इनपुट से जुड़ी होती है, जिसमें गुणवत्ता वाले बीजों तक पहुंच, बेहतर सिंचाई सुविधाएं और मृदा स्वास्थ्य में सुधार शामिल हैं।
-
पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन जैसे संबद्ध क्षेत्रों का बढ़ता महत्व, इस क्षेत्र में विविधीकरण के महत्व को रेखांकित करता है। इन क्षेत्रों का लाभ उठाकर किसान अतिरिक्त राजस्व स्रोत सृजित सकते हैं जो पारंपरिक फसल उत्पादन में अस्थिरता की स्थिति में बफर के रूप में कार्य कर सकते हैं। इस क्षेत्र की चुनौतियों में जलवायु परिवर्तन और पानी की कमी शामिल हैं।
उद्योग
-
बिजली और निर्माण क्षेत्रों में मजबूत वृद्धि के कारण 2024-25 में औद्योगिक क्षेत्र में 6.2% की वृद्धि हुई। 2024-25 की दूसरी तिमाही में औद्योगिक वृद्धि घटकर 3.6% हो गई जिसके निम्नलिखित कारण हैं: (i) तीव्र व्यापार प्रतिस्पर्धा और प्रमुख व्यापारिक देशों की औद्योगिक नीतियों के कारण मैन्यूफैक्चरिंग निर्यात में मंदी, और (ii) मानसून के असामान्य स्तर के कारण खनन और निर्माण जैसी गतिविधियों का सुस्त होना।
-
राज्य के कुल औद्योगिक सकल मूल्य वर्धन में गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु का हिस्सा लगभग 43% है। दूसरी ओर छह पूर्वोत्तर राज्यों (सिक्किम और असम को छोड़कर) का हिस्सा केवल 0.7% हैं। सर्वेक्षण में कहा गया है कि पूर्वोत्तर जैसे अद्वितीय भौगोलिक क्षेत्रों के लिए औद्योगिक रणनीतियों पर ध्यान केंद्रित करना जरूरी है। राज्यों को व्यवसाय संचालन को शुरू करने और बढ़ाने को आसान करना चाहिए।
-
भारत प्रमुख क्षेत्रों में महत्वपूर्ण अंतराल के साथ अनुसंधान और विकास (आरएंडडी) में पिछड़ा हुआ है। अनुसंधान एवं विकास पर वर्तमान व्यय जीडीपी का केवल 0.64% है जो कई देशों की तुलना में अपर्याप्त और कम है। सर्वेक्षण में उद्योग-अकादमिक सहयोग को बढ़ावा देने, निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाने और व्यावहारिक अनुसंधान को प्राथमिकता देने का सुझाव दिया गया है।
सेवा क्षेत्र
-
सेवा क्षेत्र 2022-23 और 2024-25 के बीच औसतन 8.3% की दर से बढ़ा है। कुल सकल मूल्य वर्धित में इसका योगदान 2013-14 में 51% से बढ़कर 2024-25 में लगभग 55% हो गया है। 2024-25 में अब तक सेवा क्षेत्र ने जीडीपी की वृद्धि में सहयोग दिया है, जब वैश्विक वस्तु व्यापार सुस्त होने से मैन्यूफैक्चरिंग प्रभावित हुई है।
-
सर्वेक्षण में कहा गया कि क्षेत्रीय विकास के लिए श्रम शक्ति का उचित तौर से दक्ष होना जरूरी है। इसके लिए सरकारी, निजी क्षेत्र और कौशल संस्थानों, सभी स्तरों पर प्रयासों की जरूरत है। इसके अलावा जमीनी स्तर पर जटिल प्रक्रियाओं, रेगुलेशंस और नियमों की समीक्षा और संशोधन करने की आवश्यकता है जो क्षेत्र के विकास में बाधा डालते हैं।
इंफ्रास्ट्रक्चर
-
विकास लक्ष्यों को पूरा करने के लिए भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर पर मौजूदा खर्च को बढ़ाने की जरूरत है। इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों पर केंद्र सरकार द्वारा पूंजीगत व्यय 2019-20 से 2023-24 तक 39% की दर से बढ़ा है। केंद्र सरकार के साथ-साथ राज्यों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा उठाए गए कदमों के बावजूद इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए अभी भी महत्वपूर्ण मांग पूरी नहीं हुई है। इसके लिए वित्त पोषण के नए तरीकों और अधिक निजी भागीदारी की जरूरत है।
-
उच्च विकास दर को बरकरार रखने के लिए अगले 20 वर्षों में इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश में तेजी लाने की आवश्यकता है। इसे केवल सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा पूरा नहीं किया जा सकता क्योंकि सरकार के विभिन्न स्तरों पर बजट संबंधी बाध्यताएं हैं। कार्यक्रम और परियोजना नियोजन, वित्तपोषण, निर्माण, रखरखाव और मुद्रीकरण में निजी भागीदारी में तेजी आनी चाहिए।
रोजगार
-
15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए वार्षिक बेरोजगारी दर 2017-18 में 6% से घटकर 2023-24 में 3.2% हो गई है। इस सुधार के साथ-साथ श्रम बल भागीदारी दर और श्रमिक जनसंख्या अनुपात में वृद्धि हुई है। स्व-रोज़गार प्राप्त श्रमिकों का अनुपात 2017-18 में 52% से बढ़कर 2023-24 में 58% हो गया, जो उद्यमिता से संबंधित गतिविधियों और लचीली कामकाजी परिस्थितियों के लिए प्राथमिकता को दर्शाता है। हालांकि नियमित/वेतनभोगी नौकरियों में श्रमिकों की हिस्सेदारी 23% से घटकर 22% हो गई है।
-
श्रम बाजार में लचीलापन बढ़ने से व्यवसायों के विकास के लिए एक सक्षम वातावरण तैयार होगा। भारत के श्रम नियम व्यवसायों पर व्यापक अनुपालन आवश्यकताओं को लागू करते हैं। माइक्रोमैनेजिंग नियम अनावश्यक प्रशासनिक बोझ पैदा करते हैं जो व्यवसाय के विकास में बाधा डालते हैं।
-
शिक्षण परिणामों और रोजगार क्षमता में सुधार पर ध्यान देने की आवश्यकता है। निम्नलिखित स्तरों पर सुधार की आवश्यकता हो सकती है: (i) बुनियादी भाषा, गणित और विज्ञान संबंधी कौशल के लिए स्कूली स्तर, और (ii) आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग जैसी नई युग की प्रौद्योगिकियों से संबंधित कौशल को शामिल करने के लिए उच्च शिक्षा स्तर।
डीरेगुलेशन
-
भारतीय कंपनियों में लघुस्तरीय प्रवृत्ति है। ऐसा करने से उन्हें संस्थागत पूंजी, कुशल प्रतिभा और प्रौद्योगिकी की सुविधा का लाभ नहीं मिल पाता। विस्तार न करने का कारण यह भी होता है कि रेगुलेटरी रडार से बाहर रहा जा सके, और श्रम एवं सुरक्षा संबंधी कानूनों की गिरफ्त से बचा जा सके। सर्वेक्षण में कहा गया है कि एमएसएमईज़ के लिए बड़े उद्यमों के मुकाबले डीरेगुलेशन ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि बड़े उद्यम आम तौर पर अनुपालन से निपटना जानते हैं। रेगुलेशंस समय के साथ व्यवसायों को शुरू करने और बढ़ने की क्षमता को नुकसान पहुंचाते हैं, और परिचालन निर्णयों की लागत में वृद्धि करते हैं।
-
भारतीय कंपनियों को रेगुलेशंस का पालन करना होता है तो कई बार विकास, निवेश और रोजगार सृजन में बाधा पहुंचती है। उदाहरण के लिए, निर्यातक फर्मों को ऑर्डर में बढ़ोतरी के साथ एक महीने में अधिक श्रम घंटे लागू करने की सुविधा होनी चाहिए। तेज़ आर्थिक विकास के लिए केंद्र और राज्य सरकारों को ऐसे सुधारों को लागू करना होगा, जिनकी मदद से छोटे और मध्यम उद्यम कुशलतापूर्वक काम कर सकें। डीरेगुलेशंस वाले क्षेत्रों में निम्नलिखित शामिल हैं: (i) भूमि, (ii) श्रम, (iii) परिवहन, और (iv) लॉजिस्टिक्स।
स्वीकरणः प्रस्तुत रिपोर्ट आपके समक्ष सूचना प्रदान करने के लिए प्रस्तुत की गई है। पीआरएस लेजिसलेटिव रिसर्च (पीआरएस) के नाम उल्लेख के साथ इस रिपोर्ट का पूर्ण रूपेण या आंशिक रूप से गैर व्यावसायिक उद्देश्य के लिए पुनःप्रयोग या पुनर्वितरण किया जा सकता है। रिपोर्ट में प्रस्तुत विचार के लिए अंततः लेखक या लेखिका उत्तरदायी हैं। यद्यपि पीआरएस विश्वसनीय और व्यापक सूचना का प्रयोग करने का हर संभव प्रयास करता है किंतु पीआरएस दावा नहीं करता कि प्रस्तुत रिपोर्ट की सामग्री सही या पूर्ण है। पीआरएस एक स्वतंत्र, अलाभकारी समूह है। रिपोर्ट को इसे प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के उद्देश्यों अथवा विचारों से निरपेक्ष होकर तैयार किया गया है। यह रिपोर्ट मूल रूप से अंग्रेजी में तैयार की गई है। हिंदी रूपांतरण में किसी भी प्रकार की अस्पष्टता की स्थिति में अंग्रेजी की मूल रिपोर्ट से इसकी पुष्टि की जा सकती है।