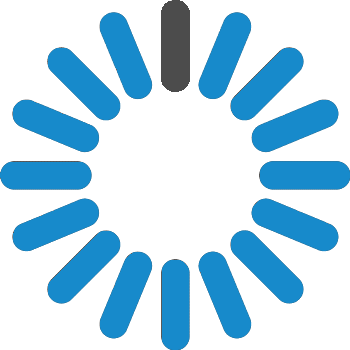स्टैंडिंग कमिटी की रिपोर्ट का सारांश
-
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस संबंधी स्टैंडिंग कमिटी (चेयर: रमेश विधूड़ी) ने ‘जैव ईंधन (बायो फ्यूल) के विशेष संदर्भ के साथ गैर परंपरागत ईंधनों के उत्पादन की प्रगति की समीक्षा’ विषय पर 10 मार्च, 2021 को अपनी रिपोर्ट सौंपी। जैव-ईंधनों को फॉसिल फ्यूल (जीवाश्म ईंधन) के आर्थिक विकल्प के तौर पर विकसित किया जाता है और इनकी प्रकृति पर्यावरण के अनुकूल होती है। इनके उदाहरणों में बायो-इथेनॉल, बायो-डीज़ल, कंप्रेस्ड बायो गैस, बायो-जेट ईंधन और दूसरे उन्नत जैव-ईंधन शमिल हैं। कमिटी के मुख्य निष्कर्षों और सुझावों में निम्नलिखित शामिल हैं:
-
राष्ट्रीय नीति: कमिटी ने गौर किया कि भारत अपना 80% से अधिक कच्चा तेल आयात करता है। ऊर्जा और परिवहन के क्षेत्रों में जैव ईंधन के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए 2018 में राष्ट्रीय जैव-ईंधन नीति बनाई गई थी। इसका लक्ष्य फॉसिल फ्यूल का स्थान लेना और ऊर्जा सुरक्षा एवं जलवायु परिवर्तन शमन में योगदान देना है। इस नीति के अंतर्गत सरकार बायोमास और कृषि अवशेषों (रेसेड्यूज़) एवं उत्पादों को कच्चे माल के तौर पर इस्तेमाल करके जैव ईंधनों का उत्पादन करेगी। इसका यह लक्ष्य भी है कि किसानों को बेहतर क्षतिपूर्ति मिले और कचरा प्रबंधन से संबंधित चुनौतियों को हल किया जा सके। इन विविध लक्ष्यों को देखते हुए कमिटी ने सुझाव दिया कि इस नीति की समय समय पर समीक्षा की जानी चाहिए ताकि संभावित समस्याओं को हल किया जा सके और नीति का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जा सके।
-
इथेनॉल ब्लेंडिंग: सरकार ने इथेनॉल की पेट्रोल के साथ ब्लेंडिंग के लिए निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए हैं: (i) 2022 तक 10% ब्लेंडिंग, और (ii) 2030 तक 20% ब्लेंडिंग। कमिटी ने गौर किया कि 2018-19 में 188 करोड़ लीटर इथेनॉल के साथ 5% ब्लेंडिंग की गई। 20% ब्लेंडिंग के लक्ष्य को पूरा करने के लिए लगभग 900 करोड़ लीटर इथेनॉल की जरूरत होगी। सरकार 2025 तक इस लक्ष्य को हासिल करना चाहती है। इसमें से 550 करोड़ लीटर चीनी आधारित डिस्टिलरीज़ से मिलेगा, और 350 करोड़ लीटर अनाज आधारित डिस्टिरीज़ से। अब तक की प्रगति को देखते हुए कमिटी ने सुझाव दिया कि 20% इथेनॉल ब्लेडिंग के लक्ष्य को आगे बढ़ा दिया जाए।
-
इथेनॉल के लिए फीडस्टॉक्स: कमिटी ने गौर किया कि ब्लेंडिंग के लिए अधिकतर इथेनॉल चीनी क्षेत्र से प्राप्त होता है। उसने कहा कि गन्ने की फसलों के लिए अधिक पानी की जरूरत होती है और इसका पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसलिए इथेनॉल उत्पादन के लिए लंबे समय में यह स्थायी विकल्प नहीं है। कमिटी ने गौर किया कि विश्व में 60% से अधिक इथेनॉल का उत्पादन मक्का से होता है, जबकि भारत मुख्य रूप से चीनी का इस्तेमाल करता है। उसने सुझाव दिया कि सरकार को दूसरे फीडस्टॉक का इस्तेमाल करने वाले देशों की नीतियों का अध्ययन करना चाहिए और अपने हिसाब से उन्हें अपनाना चाहिए। कमिटी ने कहा कि मक्का और दूसरे खाद्यान्नों से इथेनॉल उत्पादन के जरिए देश भर में इथेनॉल ब्लेंडिंग में आसानी होगी। इससे परिवहन की लागत भी कम होगी, जबकि अभी इथेनॉल मुख्य रूप से चीनी उत्पादक राज्यों में बनता है। उसने सुझाव दिया कि सरकार को इथेनॉल उत्पादन के लिए इस्तेमाल होने वाले फीडस्टॉक्स को विविध बनाना चाहिए ताकि उसमें मक्का और दूसरे खाद्यान्न शामिल किए जा सकें और किसानों को उसी हिसाब से अपने उत्पादन को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए।
-
कमिटी ने गौर किया कि सरकार गन्ने से इथेनॉल उत्पादन बढ़ाने के लिए भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में खराब खाद्यान्नों को इस्तेमाल करने की योजना बना रही है। उसने कहा कि चावल का अतिरिक्त स्टॉक इथेनॉल के उत्पादन में उपयोगी साबित हो सकता है लेकिन भविष्य में सतत तरीके से ब्लेंडिंग के लक्ष्य को हासिल करने में यह मददगार साबित नहीं हो सकता। कमिटी ने सुझाव दिया कि मंत्रालय को इथेनॉल उत्पादन के लिए चावल की अनुमत मात्रा को तय करने के लिए खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के साथ मिलकर काम करना चाहिए ताकि खाद्य सुरक्षा को कोई खतरा न पहुंचे।
-
बायो-डीज़ल: सरकार ने 2030 के लिए डीज़ल के साथ बायो-डीज़ल की 5% ब्लेंडिंग का लक्ष्य रखा है। 2019-20 में 10.56 करोड़ लीटर बायो-डीज़ल के साथ ब्लेंडिंग का स्तर 0.1% से भी कम था। कमिटी ने गौर किया कि बायो-डीज़ल ब्लेंडिंग का काम, इथेनॉल ब्लेंडिंग के आस-पास भी नहीं है। उसने कहा कि बायो-डीज़ल को पूरा महत्व नहीं दिया गया, इसके बावजूद कि डीज़ल सबसे ज्यादा उपयोग होने वाला ईंधन है और इसका इस्तेमाल अधिकतर कमर्शियल और सार्वजनिक परिवहन वाहनों में होता है। उसने कहा कि बायो-डीज़ल की ब्लेंडिंग बढ़ाने से कच्चे तेल के आयात पर काफी असर होगा। कमिटी ने सुझाव दिया कि मंत्रालय को बायो-डीज़ल के उत्पादन के लिए फीडस्टॉक के स्रोतों को गंभीरता से चिन्हित करना चाहिए और इस दिशा में ठोस कदम उठाने चाहिए। कमिटी ने कहा कि भारत में उत्पादन का मुख्य स्रोत फिलहाल आयातित पाम स्टीयरिन ऑयल है। उसने कहा कि मंत्रालय इस्तेमाल किए गए कुकिंग ऑयल (यूसीओ) को विकल्प के तौर पर बढ़ावा दे रहा है और यह सुझाव दिया कि वह यूसीओ कार्यक्रम की निगरानी करने के साथ साथ एक व्यापक जागरूकता अभियान शुरू करे।
-
राष्ट्रीय जैव-ईंधन समन्वय कमिटी (एनबीसीसी): राष्ट्रीय नीति को लागू करने के लिए 14 मंत्रालयों/विभागों के प्रतिनिधियों वाली एनबीसीसी बनाई गई है। कमिटी ने सुझाव दिया कि पेय जल एवं स्वच्छता तथा वित्तीय सेवा विभागों को एनबीसीसी में शामिल किया जा सकता है, चूंकि वे इनपुट्स/ऑर्गेनिक वेस्ट प्रदान करने, तथा ब्याज सबसिडी के जरिए प्रॉजेक्ट्स के वित्त पोषण में अहम भूमिका निभाते हैं।
अस्वीकरणः प्रस्तुत रिपोर्ट आपके समक्ष सूचना प्रदान करने के लिए प्रस्तुत की गई है। पीआरएस लेजिसलेटिव रिसर्च (पीआरएस) के नाम उल्लेख के साथ इस रिपोर्ट का पूर्ण रूपेण या आंशिक रूप से गैर व्यावसायिक उद्देश्य के लिए पुनःप्रयोग या पुनर्वितरण किया जा सकता है। रिपोर्ट में प्रस्तुत विचार के लिए अंततः लेखक या लेखिका उत्तरदायी हैं। यद्यपि पीआरएस विश्वसनीय और व्यापक सूचना का प्रयोग करने का हर संभव प्रयास करता है किंतु पीआरएस दावा नहीं करता कि प्रस्तुत रिपोर्ट की सामग्री सही या पूर्ण है। पीआरएस एक स्वतंत्र, अलाभकारी समूह है। रिपोर्ट को इसे प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के उद्देश्यों अथवा विचारों से निरपेक्ष होकर तैयार किया गया है। यह सारांश मूल रूप से अंग्रेजी में तैयार किया गया था। हिंदी रूपांतरण में किसी भी प्रकार की अस्पष्टता की स्थिति में अंग्रेजी के मूल सारांश से इसकी पुष्टि की जा सकती है।