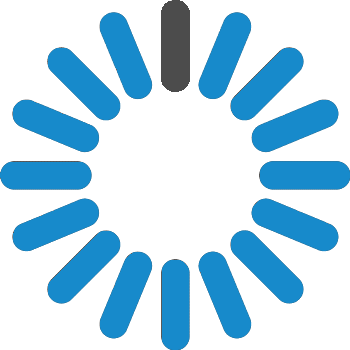स्टैंडिंग कमिटी की रिपोर्ट का सारांश
-
गृह मामलों से संबंधित स्टैंडिंग कमिटी (चेयर: डॉ. राधा मोहन दास अग्रवाल) ने 20 अगस्त, 2025 को 'साइबर अपराध: प्रभाव, संरक्षण और रोकथाम' पर अपनी रिपोर्ट पेश की। साइबर अपराध एक गैरकानूनी कृत्य है जिसमें किसी अपराध को अंजाम देने या उसे बढ़ावा देने के लिए तकनीक और डिजिटल प्रणालियों का उपयोग किया जाता है। इनमें साइबर क्षेत्र में होने वाले अपराध जैसे चोरी, धोखाधड़ी, जालसाजी, मानहानि, हैकिंग, मैलवेयर डिस्ट्रिब्यूशन और साइबर आतंकवाद शामिल हैं। कमिटी के प्रमुख निष्कर्षों और सुझावों में निम्नलिखित शामिल हैं:
-
साइबर अपराध से जुड़े व्यापक कानून: कमिटी ने कहा कि भारत में कई कानूनों में साइबर अपराध से जुड़े प्रावधान मौजूद हैं। इससे न्यायिक और प्रवर्तन संबंधी चुनौतियों पैदा होती हैं। कमिटी ने सुझाव दिया कि एक साइबर अपराध कानून बनाया जाए जो साइबर अपराधों को परिभाषित करे, उभरती प्रौद्योगिकियों से जुड़ी समस्याओं का समाधान करे और कड़े दंडात्मक प्रावधान प्रदान करे। उसने साइबर अपराधों की जांच के लिए एक इंटिग्रेटेड साइबर क्राइम टास्कफोर्स बनाने का भी सुझाव दिया।
-
आईटी एक्ट, 2000 की समीक्षा: कमिटी ने कहा कि कानून के कई प्रावधान ज़मानती हैं और उनमें कम दंड का प्रावधान है। उसने यह भी गौर किया कि कानून में निष्क्रियता के कारण पीड़ितों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए आईटी इंटरमीडियरीज़ को जिम्मेदार ठहराने का कोई प्रावधान नहीं है। उसने कानून में संशोधन का सुझाव दिया ताकि (i) कठोर दंड लगाया जा सके, (ii) आईटी इंटरमीडियरीज़ से पीड़ितों को मुआवजा देने की अपेक्षा की जा सके, और (iii) साइबर अपराध के मामलों की जांच के लिए इंस्पेक्टर के पद से ऊपर के अधिकारियों को सशक्त बनाया जा सके।
-
सीबीआई जांच के लिए राज्यों की सहमति: दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना एक्ट, 1946 के तहत राज्यों के भीतरी मामलों की सीबीआई (केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो) जांच के लिए राज्यों को अपनी सहमति देनी होगी। कमिटी ने कहा कि कई राज्यों द्वारा सहमति वापस लेने से जांच में बाधा आ रही है। कमिटी ने सुझाव दिया कि मंत्रालय उन राज्य सरकारों से परामर्श करे जिन्होंने सहमति वापस ले ली है। उसने यह भी कहा कि कानून में संशोधन किया जाए और सीबीआई को राज्य की सहमति के बिना साइबर अपराध के मामलों की जांच करने का अधिकार दिया जाए।
-
एआई कंटेंट: कमिटी ने कहा कि डीपफेक और मिसलीडिंग कंटेंट बनाने के लिए एआई का इस्तेमाल बढ़ गया है। उसने कहा कि वर्तमान में कानून यूज़र-जनरेटेड और एआई-जनरेटेड कंटेंट के बीच फर्क नहीं करता है। कमिटी ने सुझाव दिया कि एक ऐसा ढांचा बनाया जाए जो कंटेंट पर वॉटरमार्किंग अनिवार्य करे।
-
एडवर्टाइजर्स और टेलीमार्केटर्स: कमिटी ने कहा कि ऑफशोर एडवर्टाइजर्स के लिए एक व्यापक वैरिफिकेशन सिस्टम बनाने की जरूरत है। उसने यह भी कहा कि अपंजीकृत टेलीमार्केटर्स से संबंधित शिकायतों में बढ़ोतरी हो रही है। मई 2025 तक ऐसी लगभग 2.1 लाख शिकायतें थीं। उसने ऐसे अपंजीकृत टेलीमार्केटर्स को ब्लॉक करने के लिए रियल-टाइम डिटेक्शन मैकेनिज़्म बनाने का सुझाव दिया। उसने सभी ब्लैकलिस्टेड टेलीमार्केटर्स का एक केंद्रीकृत डेटाबेस बनाए रखने का भी सुझाव दिया, जिसे सभी टेलीकॉम प्रोवाइडर्स के साथ साझा किया जाए।
-
वित्तीय धोखाधड़ी से संरक्षण: आरबीआई ने सभी बैंकों को अक्टूबर 2025 तक '.bank.in' डोमेन पर माइग्रेट करने का आदेश दिया था। इससे बैंकों की प्रामाणिकता की पहचान करने में मदद मिल सकती है। कमिटी ने कहा कि किसी भी बैंक ने माइग्रेशन प्रक्रिया पूरी नहीं की है और सुझाव दिया कि आरबीआई इस प्रक्रिया की निगरानी करे। उसने एक डिजिटल पेमेंट इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म शुरू करने के लिए समय-सीमा तय करने का सुझाव दिया जिससे डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम सुरक्षित रहे। कमिटी ने कहा कि केवाईसी उपायों के बावजूद म्यूल अकाउंट्स (वित्तीय धोखाधड़ी करने के लिए बनाए गए बैंक खाते) मौजूद हैं। उसने बिहेवेरियल बायोमेट्रिक्स लागू करने की संभावना तलाशने का सुझाव दिया जो असामान्य गतिविधि का पता लगाने के लिए यूज़र की टाइपिंग स्पीड या माउस मूवमेंट जैसे कंज्यूमर पैटर्न का विश्लेषण करता है।
-
अपंजीकृत फाइनांशियल इंफ्लूएंसर्स: कमिटी ने कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ऐसे फाइनांशियल इंफ्लूएंसर्स का ट्रेंड बढ़ रहा है जोकि इस क्षेत्र में गलत सूचनाएं देते हैं। कमिटी के अनुसार, सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज़ को निर्देश दिया जाए कि वे केवल सेबी में पंजीकृत फाइनांशियल इंफ्लूएंसर्स को ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सलाह देने और मार्केटिंग करने की अनुमति दें।
-
विभिन्न संगठनों के बीच समन्वय: कमिटी ने कहा कि साइबर स्पेस में ज्ञान साझा करने और क्षमता निर्माण के लिए सरकारी एजेंसियों, रेगुलेटर्स, टेक्नोलॉजी प्लेटफार्म्स और नागरिक समाज के बीच बेहतर समन्वय की जरूरत है। कमिटी ने यह सुझाव भी दिया कि: (i) ट्राई के भीतर एक्सपर्ट वर्टिकल बनाया जाए, और (ii) सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में राज्य साइबर अपराध समन्वय केंद्र स्थापित किए जाएं।
-
अंतरराष्ट्रीय समन्वय: कमिटी ने कहा कि विदेशी सर्विस प्रोवाइडर्स के मामले में महत्वपूर्ण डेटा भारत के बाहर स्टोर होता है। लेकिन ऐसा कोई वैधानिक आदेश नहीं है कि उन्हें समय पर डेटा डिसक्लोज़र करना ही होगा। कमिटी ने यह भी कहा कि स्वैच्छिक सहयोग और संधि प्रक्रियाओं पर निर्भर रहने से साइबर अपराध की जांच धीमी हो जाती है। कमिटी ने समय पर डेटा डिसक्लोज़र के लिए प्रवर्तनीय कानूनी और कूटनीतिक उपाय करने का सुझाव दिया। कमिटी ने विदेशी एजेंसियों के साथ समन्वय के लिए 24x7 इकाई स्थापित करने का भी सुझाव दिया। इसके अलावा कमिटी ने सुरक्षित और इंटरऑपरेबल इंटेलिजेंस शेयरिंग प्लेटफॉर्म विकसित करने का भी सुझाव दिया।
डिस्क्लेमर: प्रस्तुत रिपोर्ट आपके समक्ष सूचना प्रदान करने के लिए प्रस्तुत की गई है। पीआरएस लेजिसलेटिव रिसर्च (पीआरएस) के नाम उल्लेख के साथ इस रिपोर्ट का पूर्ण रूपेण या आंशिक रूप से गैर व्यावसायिक उद्देश्य के लिए पुनःप्रयोग या पुनर्वितरण किया जा सकता है। रिपोर्ट में प्रस्तुत विचार के लिए अंततः लेखक या लेखिका उत्तरदायी हैं। यद्यपि पीआरएस विश्वसनीय और व्यापक सूचना का प्रयोग करने का हर संभव प्रयास करता है किंतु पीआरएस दावा नहीं करता कि प्रस्तुत रिपोर्ट की सामग्री सही या पूर्ण है। पीआरएस एक स्वतंत्र, अलाभकारी समूह है। रिपोर्ट को इसे प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के उद्देश्यों अथवा विचारों से निरपेक्ष होकर तैयार किया गया है। यह सारांश मूल रूप से अंग्रेजी में तैयार किया गया था। हिंदी रूपांतरण में किसी भी प्रकार की अस्पष्टता की स्थिति में अंग्रेजी के मूल सारांश से इसकी पुष्टि की जा सकती है।