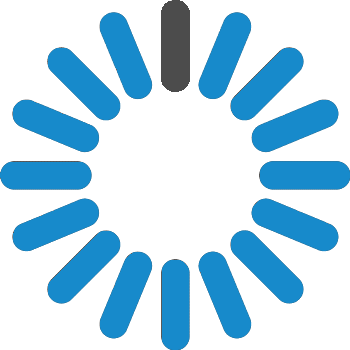दल-बदल विरोधी कानून सोमवार को फिर नाकाम साबित हुआ। इस बार यह पुडुचेरी में हुआ है। कांग्रेस-द्रमुक सरकार के मुखिया वी नारायणसामी को अपना बहुमत साबित करने के लिए कहा गया था, पर उन्होंने सदन से ‘वाकआउट’ करना बेहतर समझा। वहां पर सियासी संकट रविवार को तब गहरा गया था, जब सत्तारूढ़ गठबंधन से दो विधायकों ने इस्तीफा दे दिया और सरकार के पास सिर्फ 11 विधायकों का समर्थन रह बचा। 33 सदस्यों वाली इस विधानसभा में तीन सदस्य मनोनीत होते हैं, जबकि शेष का चुनाव जनता करती है। 2016 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 15 सीटें मिली थीं और द्रमुक को दो। मगर बीते दिनों से सत्तारूढ़ गठबंधन से (जिसमें एक निर्दलीय सदस्य भी थे) सदस्यों का इस्तीफा शुरू हुआ, जो रविवार तक जारी रहा। वी नारायणसामी ने इसका ठीकरा केंद्र सरकार पर फोड़ा है और कहा है कि उसी की शह पर सरकार गिराने की साजिश रची गई। बहरहाल, ऐसी गड़बड़ियों से पार पाने और सरकारों में स्थिरता व राजनीतिक शुचिता लाने के लिए ही संसद ने दल-बदल विरोधी कानून बनाया था। मगर 35 वर्षों की यात्रा में यह कानून अपने मकसद में पूरी तरह विफल रहा है। किसी कानून का लक्ष्य न हासिल कर पाना अपने देश में नई घटना नहीं है, पर इसका यह अर्थ नहीं है कि इसने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है। हमारी संसद और राज्य विधानसभाओं में निरर्थक बहसों के लिए यही कानून जिम्मेदार रहा है।
मसलन, लोकसभा में करीब 250 सांसदों ने अपना पेशा किसानी बताया है, वे देश भर के लोगों की नुमाइंदगी विभिन्न राजनीतिक दलों की तरफ से करते हैं। मगर नए कृषि कानूनों पर बहस के दौरान वे कृषि क्षेत्र के अपने ज्ञान और अनुभव के आधार पर इन बिलों का समर्थन या विरोध नहीं कर सके। यह कानून दरअसल, सांसदों पर राजनीतिक दलों को अपने-अपने विचार थोपने का अधिकार देता है। अगर सांसद अपनी पार्टी से अलग रुख अपनाते हैं, तो वे अपनी सीट गंवा सकते हैं। उनके पास सिर्फ एक विकल्प होता है कि वे पार्टी के विचारों को बुलंद करें और अपनी संसदीय यात्रा पूरी करें, या अपने मन की बोलें और संसद की सदस्यता गंवाने का जोखिम उठाएं।
उल्लेखनीय है कि दल-बदल विरोधी कानून न होने के कारण ही अमेरिका में सात रिपब्लिकन सीनेटरों ने अपनी ही पार्टी के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को दोषी मानने के लिए वोट दिए, जबकि दो महीने पहले ब्रिटेन में प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की पार्टी के 55 सांसदों ने लॉकडाउन को और सख्त बनाने के सरकार के प्रस्ताव के खिलाफ मत डाले थे।
दल-बदल विरोधी कानून का एक नेक मकसद सरकारों को स्थिर रखना है। मगर वर्षों से पार्टियों ने विपक्ष को कमजोर करने या फिर सरकार गिराने के लिए बतौर टूलकिट इसका इस्तेमाल किया है। विधानसभा में किसी दल के विधायकों की संख्या यदि कम है, तो वहां की बड़ी पार्टी उसके दो-तिहाई विधायकों को आसानी से अपने पाले में कर लेती है, जो इस कानून के तहत मान्य है। यदि ऐसा नहीं हो पाता, तो कुछ विधायक सरकार का समर्थन करने के लिए राजी हो जाते हैं और विधानसभा अध्यक्ष पर दबाव बनाया जाता है कि वह उनकी अयोग्यता संबंधी फैसले लेने में देरी करें। हाल के दिनों में तो विधायकों को इस्तीफा देने के लिए राजी कराने की प्रवृत्ति बढ़ी है।
हालांकि, इस बाबत अध्यक्ष के फैसलों को न्यायिक समीक्षा के दायरे में लाने संबंधी सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद ऐसे कई मामले अदालत तक भी पहुंचे हैं। मगर कभी-कभी अदालती प्रक्रिया में वक्त लगता है। जैसे शरद यादव के मामले में ही राज्यसभा के सभापति ने 2017 में तीन महीने में उनकी अयोग्यता का फैसला किया था, और यह मामला अब तक दिल्ली हाईकोर्ट में लंबित है। वैसे, राजनीतिक संकट के टलते ही ऐसे मामलों को भुला भी दिया जाता है। जैसे, पिछले महीने राजस्थान कांग्रेस के उन असंतुष्ट विधायकों की ओर से कोई भी पेश नहीं हुआ, जिन्होंने हाईकोर्ट में दल-बदल विरोधी कानून से सुरक्षा की मांग की थी। जाहिर है, चुनाव के सिर्फ तीन महीने पहले पुडुचेरी का घटनाक्रम दल-बदल विरोधी कानून की विफलता बता रहा है।
लिहाजा सवाल यही है कि आखिर कब तक यह कानून हमारे संविधान का हिस्सा बना रहेगा?
(ये लेखक के अपने विचार हैं)