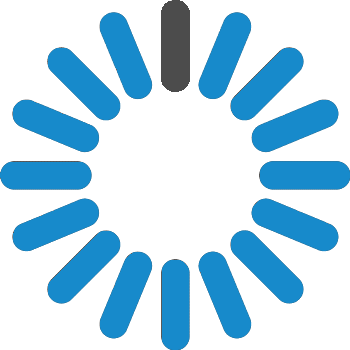स्वतंत्रता के 65 साल पूरे होने पर संसदीय लोकतंत्र के महत्वपूर्ण पड़ावों पर नजर डालना समीचीन होगा। इस संबंध में सबसे उल्लेखनीय उपलब्धि यह है कि भारतीय लोकतंत्र परिपक्व हो गया है और जहां तक संसदीय कार्यवाही का संबंध है तो यह अपेक्षाओं पर खरी उतरी है। इस बात पर खुशी मनाई जा सकती है कि सातवें दशक के एक छोटे से कालखंड को छोड़कर औपनिवेशिक दासता से मुक्त हुए देशों में भारत ही एकमात्र देश है जहां नियमित तौर पर स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होते रहे हैं। पिछले 65 वर्षो में संसद की संरचना में कुछ बदलाव हुए हैं। लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। पहली लोकसभा में कुल सांसदों में केवल पांच प्रतिशत महिलाएं थीं। यह आंकड़ा अब बढ़कर 11 फीसदी पर पहुंच गया है। यद्यपि महिला आरक्षण बिल में लक्षित आंकड़े 33 प्रतिशत से हम अभी भी काफी पीछे चल रहे हैं। सदस्यों के शैक्षिक स्तर में भी महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। 15वीं लोकसभा में 79 प्रतिशत सांसद स्नातक हैं, जबकि पहली लोकसभा में यह संख्या महज 58 फीसदी थी। वर्तमान में केवल तीन प्रतिशत सांसद माध्यमिक शिक्षा भी पूरी नहीं कर पाए हैं, 1952 में यह आंकड़ा 23 फीसदी था। अफसोस की बात यह है कि युवाओं को अधिक भागीदारी देने के नारों के बीच संसद बूढ़ी हो रही है। वर्तमान में केवल 14 फीसदी सांसद 40 साल से कम हैं, जबकि 1952 में यह आंकड़ा 26 प्रतिशत था।
कुछ मानदंडों पर संसद का प्रदर्शन साल दर साल गिरता गया। पांचवें दशक में लोकसभा की कार्यवाही साल में 120 से 140 दिनों तक चलती थी। पिछले दस वर्षो में यह संख्या 60 से 70 दिनों के बीच आ गई है। संसद में पारित होने वाले बिलों की संख्या में भी गिरावट आई है। पहली लोकसभा में प्रतिवर्ष औसतन 72 बिल पारित हुए थे, जबकि वर्तमान लोकसभा में साल में करीब 40 बिल ही पारित होते हैं। वास्तव में संसद के पिछले सत्र की समाप्ति पर लंबित बिलों की संख्या सैकड़ा पार कर गई है। इस संबंध में उल्लेखनीय है कि सांसदों (जो मंत्री नहीं हैं) की विधायी भागीदारी में भी कमी आई है। यह इस तथ्य से पुष्ट होता है कि 1970 के बाद से एक भी निजी बिल पारित नहीं हुआ है।
इस परिप्रेक्ष्य में संसदीय तंत्र को कैसे मजबूती प्रदान की जा सकती है? मेरा मानना है कि तीन परिवर्तन संसद का प्रभाव और उसकी उत्पादकता बढ़ा सकते हैं। सबसे पहली आवश्यकता यह है कि सांसदों को काम करने में सहयोग देने के लिए उन्हें उचित सहायक तंत्र से लैस करना होगा। अधिकांश उन्नत लोकतंत्रों के विपरीत भारतीय सांसदों को अनुसंधान और शोध के लिए समुचित सुविधाएं नहीं मिलती हैं। अमेरिका में एक सीनेटर को विभिन्न विषयों के विश्लेषण में सहायता प्रदान करने के लिए 15 शोधकर्ताओं का स्टाफ मिलता है। एक ब्रिटिश सांसद को तीन से पांच शोधकर्ता मिलते हैं। भारत में सांसद को स्टाफ की नियुक्ति के लिए महज 28,000 रुपये का भत्ता मिलता है। इस राशि में दो कर्मचारी मिलने भी मुश्किल हैं। इसके अलावा सांसदों को दिल्ली में कार्यालय के लिए स्थान भी नहीं मिलता। ऐसे समय जब विधायिका और नीतिगत बहसें अधिकाधिक जटिल और तकनीकी होती जा रही हैं, टेलीकॉम से लेकर ऊर्जा क्षेत्र, शिक्षा, स्वास्थ्य, रक्षा और विदेश नीति में विशेषज्ञ शोधकर्ताओं के अभाव में मुद्दे की गहराई में पहुंच पाना मुश्किल हो गया है। नागरिक अपेक्षा करने लगे हैं कि बिलों और नीतिगत मामलों में उनका सांसद सूचनाओं से लैस होकर अपना पक्ष रखेगा। बिना मजबूत शोध टीम के उनकी यह अपेक्षा पूरी होना संभव नहीं दिखता।
दूसरी आवश्यकता है सांसदों के मतदान के रिकॉर्ड को पारदर्शी रखना। भारतीय संसद में अधिकांश बिल तथा अन्य प्रस्ताव ध्वनि मत से पारित कर दिए जाते हैं। स्पीकर किसी मुद्दे के पक्ष में सांसदों को ‘आई’ और विरोध में ‘नो’ कहने के लिए बोलते हैं। ध्वनि मत के आधार पर स्पीकर अपने विवेक से फैसला कर देते हैं कि किसके पक्ष में सांसदों की संख्या अधिक है। अगर कोई सांसद स्पीकर के फैसले को चुनौती देता है तो फिर वोटिंग उपकरण के जरिये मतदान करा लिया जाता है। ध्वनि मत की एक बड़ी कमी यह है कि इसके माध्यम से हुए मतदान में नागरिकों को यह पता नहीं चल पाता कि किसी सांसद ने पक्ष में मतदान किया है या विपक्ष में। संसद में वोटिंग उपकरण के माध्यम से मतदान की व्यवस्था एक महत्वपूर्ण सुधार होगा। इससे नागरिक अपने प्रतिनिधियों के रिकॉर्ड पर निगाह रख सकते हैं। इससे जनप्रतिनिधि अपने निर्वाचन क्षेत्र में मतदान के फैसले को न्यायोचित ठहरा सकता है। यह देखते हुए कि संसद में प्रत्येक सांसद की सीट पर इलेक्टॉनिक वोटिंग उपकरण लगा दिया गया है, इस परिवर्तन को लागू करना बेहद सुगम होगा। असलियत में, दलबदल विरोधी कानून लागू होने के बाद से सांसद अपने विवेक से वोट देने के लिए स्वतंत्र नहीं रह गए हैं। यह सुधार का तीसरा मुद्दा है। सरकार की अस्थिरता पर अंकुश लगाने के लिए 1985 में संविधान संशोधन के माध्यम से दलबदल विरोधी कानून लागू किया गया था। इस कानून के तहत यदि कोई सांसद या विधायक अपनी पार्टी द्वारा जारी किए गए व्हिप का उल्लंघन कर मतदान करता है तो उसकी सदस्यता रद हो जाएगी। इस कानून के कारण हर सांसद को अपनी पार्टी की लाइन के अनुसार वोट देना जरूरी हो गया है। इस नियम का नुकसान यह हुआ कि सांसदों को अपने विवेक के आधार पर मतदान करने का अधिकार नहीं रह गया है। इसका यह भी तात्पर्य है कि यदि पार्टी के फैसले के कारण सांसद के निर्वाचन क्षेत्र पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है तो वह क्षेत्रीय हितों की सुरक्षा नहीं कर पाएगा।
सरकार की स्थिरता के सवाल की अहमियत से इन्कार नहीं किया जा सकता, लेकिन बहुत से मुद्दे ऐसे हैं जिन पर सांसदों की राय की स्वतंत्रता से सरकार की स्थिरता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। दुर्भाग्य से दलबदल विरोधी कानून ने इन मुद्दों पर भी सदस्य की स्वतंत्रता का हनन कर दिया है। स्थिरता और जनप्रतिनिधित्व के बीच टकराव को टालने के लिए कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने महत्वपूर्ण सुझाव दिया है कि दलबदल विरोधी कानून को केवल अविश्वास प्रस्ताव तथा वित्तीय बिलों तक सीमित कर दिया जाए। भारत की विविधता और जटिलता देखते हुए केवल संकल्पित लोकतंत्र ही परस्पर टकराने वाले हितों के बीच समान धरातल की तलाश कर सकता है। हमें दो चुनावों के बीच के कालखंड के लिए नागरिकों और सांसदों के बीच बेहतर संपर्क की भी जरूरत है। हमारी संसदीय प्रक्रियाओं में कुछ अहम परिवर्तनों से संसद की प्रभावोत्पादकता का महत्वपूर्ण रूपांतरण हो सकता है।
(लेखक शोध संस्था पीआरएस लेजिस्लेटिव के प्रमुख हैं )